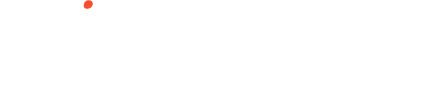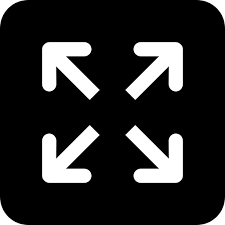फेक न्यूज के सरदर्द के खिलाफ एकजुट हो रही है दुनिया
रूस की संसद ने फेक न्यूज से निबटने के लिए कानून बनाने की तैयारी कर ली है। भारत में भी सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से फेक न्यूज के खिलाफ कदम उठाने को कहा है। केन्या, मलेशिया और जर्मनी फेक न्यूज के खिलाफ कानून बना चुके हैं। सिंगापुर, फिलीपींस और फ्रांस अपने यहां कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं।
 Alok Singh Bhadouria 24 July 2018 9:01 AM GMT
Alok Singh Bhadouria 24 July 2018 9:01 AM GMT

फेक न्यूज ने दुनिया भर के देशों को परेशान कर रखा है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक छोटी सी अफवाह राज्यों की कानून-व्यवस्था, समाज के भाईचारे और देशों की एकता-अखंडता को हिलाकर रख देगी। फेक न्यूज ने यही काम किया है। सूचना क्रांति के परों पर सवार होकर सोशल मीडिया पर फैली एक छोटी सी अफवाह पलक झपकते ही अफवाहों के चक्रवात में बदल जाती है। भारत ही नहीं दुनिया के बहुत सारे देश फेक न्यूज के सिरदर्द से परेशान हैं मसलन नाइजीरिया, केन्या, यूगांडा, तनजानिया, मैक्सिको वगैरह। रूस की संसद ने फेक न्यूज से निबटने के लिए कानून बनाने की तैयारी कर ली है। भारत में भी सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से फेक न्यूज के खिलाफ कदम उठाने को कहा है।
रूस में आएगा नया कानून
वैसे तो रूस पर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने आरोप लगाए थे कि 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में रूस ने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की थी, लेकिन अब खुद रूस फेक न्यूज से परेशान होकर सोशल मीडिया कंपनियों पर कानूनी शिकंजा कसने वाला है। हाल ही में रूस की संसद में सत्तारूढ़ दल युनाइटेड रशिया ने एक विधेयक पेश किया है जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके दायरे में ऐसी वेबसाइट आएंगी जिन पर रोज एक लाख से ज्यादा विजिटर आते हैं और कमेंट करते हैं। प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि किसी आपत्तिजनक बयान की शिकायत करने के 24 घंटे बाद भी उसे नहीं हटाया गया तो वेबसाइट कंपनी को 5 करोड़ रूबल या लगभग 5.5 करोड़ रुपए का हर्जाना देना होगा। इसके अलावा इन कंपनियों को अपने दफ्तर रूस में भी खोलने होंगे ताकि सुरक्षा एजेंसियों के साथ ठीक से तालमेल बैठा सकें।
Russia introduces bill cracking down on "fake news" https://t.co/AlEWj16LDB pic.twitter.com/ECy7i8nPvK
— The Hill (@thehill) July 24, 2018
केन्या ने बनाया सख्त कानून
केन्या में फेक न्यूज से निपटने के लिए एक कानून लाया गया है जिसके तहत फर्जी खबरें पोस्ट करने वाले पर 50 हजार डॉलर का जुर्माना और दो साल की कैद का प्रावधान है। लेकिन इस कानून का जनता और मीडिया संगठनों ने यह कहकर विरोध किया है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन होता है।
केन्या के अलावा मलेशिया मार्च में, जर्मनी जनवरी में फेक न्यूज के खिलाफ कानून बना चुके हैं। सिंगापुर, फिलीपींस और फ्रांस अपने यहां कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं।
मैक्सिको में अनूठी पहल
मैक्सिको में 1 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव हुए। चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा में लगभग 130 लोग मारे जा चुके थे। डर था कि चुनाव वाले दिन और हिंसा होगी और इससे परिणाम भी प्रभावित हो सकते हैं। इससे निपटने के लिए मीडिया ग्रुप अल जजीरा ने एक अनोखी पहल की। उसने करीब 90 संगठनों, (जिनमें पब्लिशर्स, मीडिया ग्रुप, एनजीओ, यूनिवर्सिटी शामिल हैं) के साथ "वैरिफिकैडो" नाम का एक साझा मंच तैयार किया साथ ही चुनाव पर नजर रखने के लिए फेसबुक और गूगल को भी अपने साथ लिया है। वैरिफिकैडो ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक सर्च टूल बनाया है जिसे नाम दिया है क्रिजाना। क्रिजाना ने मतदान के दौरान फैलने वाली फेक न्यूज पर नजर रखी और यूजर को आगाह किया कि फलां खबर झूठी है ताकि लोग अफवाहों पर भरोसा न करके अपने विवेक से वोट दें।
नाइजीरिया में फेक न्यूज का आतंक
अभी हाल ही में अफ्रीकी देश नाइजीरिया में सोशल मीडिया पर फैली सांप्रदायिक दंगों की झूठी तस्वीरों से देश में तनाव और आतंक का माहौल बन गया। नाइजीरिया में कुछ समय पहले मुस्लिम पशु चराने वालों और ईसाई किसानों के बीच हुए संघर्ष में 200 लोग मारे गए थे। इसके कुछ दिन बाद से सोशल मीडिया पर इस घटना में घायल लोगों और उन पर हुए अत्याचारों के कथित फोटो वायरल होने लगे। इन फोटो को ट्विटर पर सैकड़ों बार रिट्वीट भी किया। इससे तनाव फिर पनपने लगा, जबकि असलियत यह थी कि ये फोटो 2011 में हुई एक घरेलू हिंसा के थे। इसी तरह एक और फोटो वायरल हुई जिसमें बताया गया था कि हमले में आधा दर्जन लोग मारे गए। जब फोटो की जांच हुई तो पाया गया कि यह फोटो तो नाइजीरिया की थी ही नहीं बल्कि एक दूसरे देश डोमिनिकन रिपब्लिक में 2015 में हुई एक सड़क दुर्घटना की थी। बात केवल फर्जी फोटो तक ही नहीं रुकी, इसी सप्ताह नाइजीरिया के प्रमुख मीडिया संस्थानों ने एक खबर चलाई जिसमें पशु चराने वालों से जुड़े एक संगठन के प्रमुख डनलाडी सिरकोमा के हवाले से हमलों को वाजिब ठहराया गया था। इससे फिर समाज में गुस्सा और तनाव फैलने लगा, जबकि सिरकोमा ने इस तरह के किसी भी बयान से इनकार किया। जनवरी में किसी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति का फेक ट्विटर अकाउंट बनाकर पशु चराने वालों की हिंसा को जायज भी ठहराया था। चूंकि राष्ट्रपति पशु चराने वाले समाज से हैं इसलिए जनता में तीखी प्रतिक्रिया हुई। आनन-फानन में राष्ट्रपति को सफाई देनी पड़ी। फरवरी में एक और चेतावनी वायरल हुई कि देश के मुख्य एक्सप्रेसवे पर पशु चराने वाले हमला करने वाले हैं, स्थानीय पुलिस ने तुरंत इसका खंडन किया और हालात काबू में आए ।
यह भी देखें: ज्ञानी चाचा और भतीजे ने सिखाया फेक न्यूज और सच्ची खबर का भेद
अशिक्षा, सरकार व जनता के बीच संवादहीनता और सस्ते स्मार्टफोन का घातक मेल
फेक न्यूज से परेशान नाइजीरिया, केन्या, यूगांडा, तनजानिया और मैक्सिको जैसे देशों व भारत में कई समानताएं हैं जो फेक न्यूज के पैदा होने के लिए जिम्मेदार हैं। इन सभी देशों में बहुत बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं जैसे 18.6 करोड़ लोगों की तादाद वाले देश नाइजीरिया में करीब 2.6 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। नाइजीरिया में शिक्षा का स्तर भी बहुत ज्यादा नहीं है लगभग 59 फीसदी है। इसके अलावा यहां सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर ढेरों विभिन्नताएं और उनसे संबंधित समस्याएं हैं जिन्हें ये अफवाहें हवा देती रहती हैं। सस्ते स्मार्टफोन की उपलब्धता और सरकार व समाज केबीच संवाद की कमी छोटी सी अफवाह को भयानक आंधी में तब्दील कर देते हैं।
कैंब्रिज यूनिवर्सिटी ने बनाया गेम
"जादूगर के जादू को समझने के लिए हमें पहले जादू सीखना पड़ता है," यह कहना है ब्रिटेन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के सोशल डिसिजन मेकिंग लैब के डायरेक्टर डॉ. सैंडर वानडर लिन्डेन का। फेक न्यूज से लड़ने के लिए कैंब्रिज विश्वविद्यालय ने एक गेम बनाया है। इस गेम के जरिए यूजर देखता है कि कैसे फेक न्यूज बनाने वाले चर्चित लोगों, अखबारों व वेबसाइटों के फर्जी अकाउंट बनाते हैं; उनसे कैसे फर्जी संदेश या अफवाहें पोस्ट करते हैं और फिर कैसे उनके फॉलोअर बढ़ते जाते हैं। इस गेम का नाम है 'बैड न्यूज'। डॉ. सैंडर का कहना है, "जब आप पहली बार जादू देखने जाते हैं तो ठगे जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि जादूगर ने ऐसा किया कैसे। इस गेम के जरिए हम लोगों को यही बताते हैं कि फेक अकाउंट, झूठी खबरें बनाई कैसे जाती हैं ताकि आप उन्हें पहचानना सीख जाएं।"
सोशल मीडिया कंपनी जैसे फेसबुक और ट्विटर ने फेक न्यूज पहचानने के कुछ टिप्स भी दिए हैं :
1. खबर के सोर्स को जांचें : खबर पढ़ने वाला जांचे कि क्या खबर किसी फेक अकाउंट से पोस्ट की गई है। अगर किसी समाचार एजेंसी ने पोस्ट की है तो क्या वह सही है? अक्सर इन पोस्ट के साथ लिखा होता है, " मुख्य धारा का मीडिया आपको सच नहीं बताएगा …" अगर ऐसा देखें तो इनकी सचाई जांचे बगैर न भरोसा करें न शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ब्लू टिक वगैरह के जरिए बताते हैं कि किसी मशहूर हस्ती, पार्टी या संगठन का सोशल मीडिया अकाउंट वेरिफाइड है या नहीं। आपको इससे मदद मिल सकती है।
2. देखें यही खबर कहीं और चल रही है क्या : हालांकि ऐसा करने में भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें क्योंकि जरूरी नहीं जहां आप जांच रहे हों वह सोर्स सही हो। फिर भी अगर कोई बड़ी खबर होगी तो कहीं और जरूर चली होगी, इस नियम को मानकर चलें।
3. वेरिफिकशन टूल्स का इस्तेमाल करें : किसी फोटो या विडियो को परखने के लिए अपने इंटरनेट ब्राउजर पर रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल करें। विडियो का स्नैपशॉट लेकर उसे इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं।
4. शेयर करने से पहले कई बार सोचें : आखिर में जो सबसे जरूरी चीज है वह है आपका अपना विवेक। कोई भी खबर शेयर करने से पहले पूरी तरह से निश्चिंत हो लें कि वह सही है भी या नहीं। एक बार खुद से यह भी पूछ लें कि क्या इसे शेयर करना जरूरी है क्योंकि एक अफवाह शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है और लोगों की मौत की वजह भी साबित हो सकती है।
यह भी देखें: गाँव कनेक्शन और फेसबुक की मुहिम 'मोबाइल चौपाल'... हम बता रहे हैं कैसे करें इंटरनेट का सही उपयोग
गांव कनेक्शन की मोबाइल चौपाल
इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल और सोशल मीडिया पर फैलने वाली फेक न्यूज के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए गांव कनेक्शन ने एक अनोखी मुहिम चलाई है। गांव कनेक्शन ने फेसबुक के साथ मिलकर युवाओं, खासकर ग्रामीण युवाओं को ध्यान में रखकर मोबाइल चौपाल नामका एक अभियान शुरू किया है। इसमें "गांव रथ" नामके एक सचल वाहन के जरिए अलग-अलग स्थानों पर जादू, संगीत और दूसरे रोचक माध्यमों के जरिए लोगों को जागरुक किया जा रहा है।
More Stories