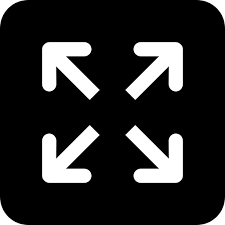कोरोना काल में 'विपरीत पलायन' का दंश झेलते प्रवासी मज़दूरों की गाथा
बेहतर आजीविका, रोज़गार और जीवनशैली की तलाश में अपने गांव, नगर, देश से अन्य स्थानों तक लोगों का जाना और वहाँ काम करना कोई नई बात नही है। सभ्यता का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है।
 Sushil Kumar 4 Jun 2020 7:13 AM GMT
Sushil Kumar 4 Jun 2020 7:13 AM GMT

बेहतर आजीविका, रोज़गार और जीवनशैली की तलाश में अपने गांव, नगर, देश से अन्य स्थानों तक लोगों का जाना और वहाँ काम करना कोई नई बात नही है। सभ्यता का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है।
सामान्य तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों के जाने को 'प्रवास' की संज्ञा दी जाती है। परन्तु ऐसी परिस्थितियों में जब लोगों के पास अपने जीवन-यापन के लिए न चाहते हुए भी घर-बार, सगे-सम्बन्धी, नाते-रिश्तेदार छोड़ कर परदेश जाने के सिवाय कोई और चारा नही होता है तब समाज विज्ञान की शब्दावली में इसको 'पलायन' के रूप में चिन्हित किया जाता है। एक सीमा तक प्रवास स्वैछिक होता है जबकि पलायन किसी ना किसी रूप में थोपा गया होता है, भले ही ऐसा किसी परिस्थिति, व्यक्ति या सरकार द्वारा किया गया हो।
आज़ादी के पहले, जब औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन भारत में अपनी जड़ें जमा कर भारत के साथ-साथ भारत के बाहर भी अपने औद्योगिक केन्द्रों और कृषि क्षेत्रों को विकसित करने लगा था, 'प्रवास' की जगह 'पलायन' का फलक एक अमानवीय वास्तविकता का रूप लेने लगा था। उस दौरान संयुक्त बंगाल के आज के बिहार और बिहार की सीमाओं से लगते हुए उत्तर प्रदेश के गाँवों से तब के एक बड़े प्रशासनिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक केन्द्र कलकत्ता की ओर लम्बे समय तक श्रम-शक्ति का 'प्रवास' और 'पलायन' होता रहा। उसी अवधि में ब्रिटिश शासन द्वारा तथाकथित 'एग्रीमेन्ट' के सहारे बड़ी संख्या में भारत के लोगों को ब्रिटिश कैरिबियाई उपनिवेशों में खेतों और मिलों में मज़दूरों के रूप में काम करने के जबरिया ले जाया गया। उन भारतीय किसानों एवं खेतिहर मज़दूरों को जनसामान्य में 'गिरमिटिया' मज़दूरों के रूप में जाना गया।
समुद्री मार्ग से ले जाए उन भारतीयों की त्रासद कहानियाँ आज भी शरीर में झुरझुरी पैदा कर देती हैं। भारत से कैरिबियाई उपनिवेशों तक की उनकी यात्रा और वहाँ जिन अमानवीय परिस्थितियों में उनको रहना, काम करना और जीना पड़ा वो एक सीमा तक अफ्रीकी अश्वेत दासों की हृदय-विदारक कहानियों से मेल खाता है। उनके जबरिया स्थानान्तरण को प्रवास, उत्प्रवास या पलायन या ऐसे किसी भी अन्य शब्दों के ज़रिए स्पष्ट नही किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें : श्रम कानूनों में बदलाव का विश्लेषण क्यों जरूरी है?
मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब स्वयं मनुष्यों द्वारा लाई गई आपदाओं को परिभाषित करना मुश्किल रहा है। आज का वैश्विक कोरोना संकट कुछ ऐसा ही है। इसके दंश झेल रही मानवता अभी तक हतप्रभ हो इसकी त्रासदी को देखने और इससे बचने के ऐसे-वैसे उपाय करने के सिवाय कुछ कर नहीं पा रही है।
तब की स्वार्थी एवं शोषक ब्रिटिश सत्ता ने ऐसी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ निर्मित की जिनमें फँस कर गरीबों और साधनहीनों ग्रामीणों के एक बहुत बड़े वर्ग को अपना सब कुछ पीछे छोड़ कर जीवन को किसी तरह जीते रहने की उम्मीद लिए शहरी और नव-स्थापित औद्योगिक केन्द्रों को पलायन करना पड़ा था। अविभाजित बंगाल के अकाल-दुकाल, समय-समय पर आई ऐसी अन्य आपदाओं और इनके कुप्रबन्धन के कारण भी लाखों जीवित बच गए लोगों के मन में घर कर गए असुरक्षा के भाव ने भी ऐसे पलायनों को बल दिया।
वह भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक-आर्थिक उथल-पुथल का एक कठिन दौर था जिसमें पलायन की विभीषिका ने हमारी सामाजिक संस्कृति में 'रेलिया बैरन पिया को लिए जाए', 'बज्जर पड़े ऐसी नोकरिया पर' और 'परदेसी बलमुआ' जैसे मुहावरे गढ़े, बिदेसिया जैसे साहित्यिक प्रतिमान स्थापित किए और पलायन एवं प्रवास को एक सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता के रूप में हमारे सामने ला कर एक तरह से पटक दिया।
आज़ादी के बाद भी नागरिकों के प्रवास और पलायन के संदर्भ में कभी कुछ सकारात्मक परिवर्तन आया हो, ऐसा विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता है। बल्कि आजादी के बाद के भारत में लागू किए गए आर्थिक विकास के प्रारूपों का यदि विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत केन्द्रीकृत औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं नगरीय विकास ने ग्रामीण-नगरीय सातत्य को चोट पहुँचाने के साथ-साथ ग्रामीण-नगरीय भेद को भी निरन्तर बढ़ाया ही है।
यह भी पढ़ें : प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर क्यों आंख मूंद लेती हैं सरकारें?
आज़ादी के बाद भी नागरिकों के प्रवास और पलायन के संदर्भ में कभी कुछ सकारात्मक परिवर्तन आया हो, ऐसा विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता है। फोटो साभार : डाउन टू अर्थ
विभिन्न कारणों से संयुक्त परिवारों के बिखराव, कृषि जोतों के औसत आकार में निरन्तर आई कमी, खेती में लाभ के अभाव, जनसंख्या में अनियंत्रित बढ़ोतरी, ग्रामीण एवं वन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि और इनके समानान्तर औद्योगिक एवं नगरीय केन्द्रों के विकास ने ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को आजीविका और रोजगार के संदर्भ में अपनी ओर आकर्षित किया।
दीर्घावधि में इसका परिणाम यह हुआ कि औद्योगिक एवं नगरीय क्षेत्रों में क्रमश: कामचलाऊ बस्तियाँ बसने लगीं, अधिकतर झुग्गी-झोपड़ियों और गंदी बस्तियों के रूप में। मुम्बई की धारावी, दिल्ली की काली बस्ती और प्रायः प्रत्येक औद्योगिक केन्द्र में इनका एक अमानवीय प्रारूप विकसित हुआ देखा जा सकता है।
निश्चित तौर पर ये बस्तियाँ प्रवासी मज़दूरों एवं कामगारों को रहने के लिए कोई आदर्श आवास प्रदान नही करती हैं बल्कि दिन में काम कर के रोजी-रोटी कमाने वाले ये लोग इनमें अगली सुबह तक के लिए किसी प्रकार अपनी रातें काटते हैं। इनमें ना तो दैनिक जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं और ना ही पारिवारिक और नारी जीवन की गरिमा को बनाए रख सकने वाला वातावरण होता है।
बावजूद इसके इनमें मज़दूरों, कामगारों, रेहड़ी वालों, रिक्शा चालकों, कूड़ा बीनने वालों और जीवीकोपार्जन के ऐसे ही अन्य छोटे-मोटे अस्थाई प्रकृति के कामों को करने वाले लोग रहने को विवश होते हैं तो जिन आर्थिक परिस्थितियों से ग्रस्त एवं त्रस्त हो कर उन्होंने अपने घर-गाँव छोड़े होंगे, उसकी सहज कल्पना की जा सकती है।
यह भी पढ़ें : मजदूरों का रिवर्स पलायन: कुछ ने कहा- परदेस वापिस नहीं जाएंगे, कुछ ने कहा- मजबूरी है!
औद्योगिक एवं नगरीय क्षेत्रों में कामचलाऊ बस्तियाँ बसने लगीं, अधिकतर झुग्गी-झोपड़ियों और गंदी बस्तियों के रूप में।
एक ऐसे समय को जिसको आने वाली पीढ़ियाँ इतिहास के पन्नों के माध्यम से 'कोरोना-काल' के रूप में जानेंगी, श्रमिकों और कामग़ारों के घर वापसी की विचलित कर देनी वाली तस्वीरें 'परतन्त्र' और 'स्वतन्त्र' भारत के बीच के अन्तर को रेखांकित करने के लिए कत्तई संदर्भित नहीं की जा सकेंगी।
विकास की एक लम्बी यात्रा तय करने के बावज़ूद प्रतिवर्ष बढ़ते हुए आँकड़े देश के निर्धनों और वंचितों के एक बड़े वर्ग के श्रम के प्रति सम्मान का वातावरण बना सकने में सफल नही हो पाए हैं। राजनीति के सामाजिक न्याय के विफ़ल संस्करणों ने प्रायः आधे से ज्यादा भाग में राजनीतिक अवसरवाद और अस्थिरता की ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दिया है जिसने आमजन को दर-दर भटकाना जारी रखा है।
अपनी जड़ों से बिछड़े लोग प्रवासी मज़दूर तो बन गए पर प्रत्येक उथल-पुथल उनको उनके घरों की ओर धकेलती नज़र आती है। चाहे पश्चिम बंगाल का 'सातू खोर' सिन्ड्रोम हो या महाराष्ट्र का 'भईया' सिन्ड्रोम, इन सब से त्रस्त होता रहा प्रवासी मज़दूर वर्ग आज व्यापक स्तर पर कोरोनाजन्य देशव्यापी लॉकडाउन में इन पुरानी त्रासदियों को ही भोग रहा है परन्तु कहीं अधिक त्रासद एवं अमानवीय स्तर पर।
उस पर तुर्रा यह कि इसके लिए किसी व्यक्ति, दल या राज्य विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। माना कि कोविड-19 एक घोषित महामारी है परन्तु अपने हाल पर छोड़ दिए गए असहाय मज़दूरों की दुर्दशा के लिए क्या कोविड-19 और स्वयं मज़दूरों के सिवाय क्या कोई और जिम्मेदार नहीं है?
(डॉ. सुशील कुमार स्वतंत्र पत्रकार और लेखक हैं)
यह भी पढ़ें : सरकारी आश्वासनों के बाद भी सड़कों पर प्रवासी मजदूरों की पैदल यात्रा जारी है
More Stories