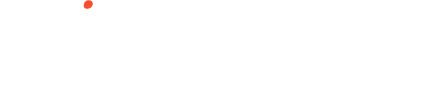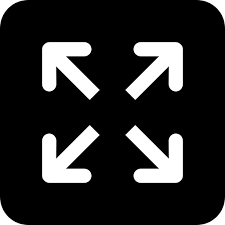उत्तर प्रदेश में क्यों घट गया सरसों की खेती का क्षेत्रफल?
 Divendra Singh 21 Jan 2020 12:16 PM GMT
Divendra Singh 21 Jan 2020 12:16 PM GMT
 साल 1996-97 में उत्तर प्रदेश में 12 लाख हेक्टेयर में सरसों की खेती होती थी, जो साल 2016-17 में 6.9 लाख हेक्टेयर रह गया।
साल 1996-97 में उत्तर प्रदेश में 12 लाख हेक्टेयर में सरसों की खेती होती थी, जो साल 2016-17 में 6.9 लाख हेक्टेयर रह गया।लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। "दस-बारह साल पहले हमारे यहां करीब दस एकड़ में सरसों की खेती होती थी, अब हम सिर्फ आलू और गेहूं की खेती करते हैं। सरसों की खेती के साथ बहुत सी परेशानियां हैं। "मथुरा जिले के बलदेव ब्लॉक के किसान रवींद्र कहते हैं। रवींद्र भी उत्तर प्रदेश के उन किसानों में से एक हैं, जिन्होंने सरसों छोड़ दूसरी फसलों की खेती शुरू कर दी।
सरसों अनुसंधान निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार 25 साल पहले सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान था, जबकि अब राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों में आगरा और मथुरा का पहला और दूसरा स्थान है। "पहले हमारे यहां तो इस समय दूर-दूर तक सिर्फ सरसों के ही खेत दिखाई देते थे, लेकिन अब लोग गेहूं-आलू उगाते हैं, "रवींद्र आगे कहते हैं।
उत्तर प्रदेश में 1981-82 में सरसों का क्षेत्रफल 22.76 लाख हेक्टेयर था, जोकि पूरे देश के सरसों की खेती के क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत था, लेकिन सरसों के क्षेत्रफल में लगातार गिरावट आती रही। सरसों के घटते क्षेत्रफल और उत्पादन के बारे में सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर, राजस्थान के निदेशक डॉ. पीके राय कहते हैं, "अगर आप आज के 25 साल पहले देखेंगे तो सरसों उत्पादन में यूपी का पहला स्थान था, लेकिन ज्यादा उत्पादन वाली गेहूं की नई किस्मों के आने से गेहूं का क्षेत्रफल बढ़ता गया। लोगों का रुझान सरसों से घट यूपी से ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होने लगा।"
साल 1996-97 में उत्तर प्रदेश में 12 लाख हेक्टेयर में सरसों की खेती होती थी, जो साल 2016-17 में 6.9 लाख हेक्टेयर रह गया।
उत्तर प्रदेश और देश में सरसों का उत्पादन और क्षेत्रफल
| अवधि | उत्तर प्रदेश | देश | ||||
| क्षेत्रफल | उत्पादन | लाभ | क्षेत्रफल | उत्पादन | लाभ | |
| 1980-81 से 1989-90 | -8.10 | -3.64 | 4.86 | 2.13 | 6.71 | 4.48 |
| 1990-91 से 1999-00 | -0.66 | -0.23 | 0.43 | 0.46 | 1.14 | 0.67 |
| 2000-01 से 2009-10 | -4.70 | -3.57 | 1.19 | 2.46 | 5.14 | 2.63 |
| 2010-11 से 2016-17 | -0.37 | -3.40 | -3.05 | -2.11 | -0.56 | 1.60 |
| 1980-81 से 2016-17 | -3.67 | -1.96 | 1.77 | 1.09 | 3.49 | 2.38 |
वो आगे कहते हैं, "सरसों के उत्पादन घटने के पीछे दरअसल एक ही नहीं कई कारण थे। एक तो जिस तरह से गेहूं का एमएसपी बढ़ती गई, उस तरह से सरसों का नहीं बढ़ा है। अब जाकर सरकार ने कुछ ध्यान दिया है तो कुछ एमएसपी बढ़ी है। अगर आप पिछले के कई साल देखेंगे तो सरसों की एमएसपी पर ध्यान ही नहीं दिया गया।"
खाद्य तेलों का आयात भी एक प्रमुख कारण है। खाद्य तेल वर्ष 2018-19 (नवंबर-18 से अक्टूबर-19) के दौरान 149.13 लाख टन का हुआ है जबकि इसके पिछले तेल वर्ष में आयात 145.16 लाख टन का हुआ था। तेल वर्ष 2016-17 में देश में रिकार्ड 150.77 लाख टन का हुआ था। उद्योग के अनुसार खाद्य तेलों के आयात पर सालाना करीब 70,000 करोड़ रुपये का खर्च हो रहा है। "कुछ पॉलिसी के इश्यू थे जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी भी घटती गई, जो बाहर से तेल इंपोर्ट होता है, उस पर ड्यूटी घटाते-घटाते जीरों कर दी गई, इससे देश में तेल मंगाना आसान हो गया। खासकर जो मलेशिया और इंडोनेशिया तो पॉम ऑयल आता था वो काफी सस्ता पड़ता था। इससे किसान भी तिलहन की खेती से पीछे हटते चले गए। ये सारे तिलहनी फसलों के साथ हुआ, इसी में सरसों भी था, "डॉ पीके राय ने आगे कहा।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के रवि पाल अब सिर्फ गेंदा की खेती करते हैं। वो कहते हैं, "अब तो सिर्फ अपने काम भर के लिए सरसों की खेती करते हैं, दस साल पहले करीब दस बीघा में ही सरसों की खेती होती थी, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं, इसलिए तो अब हम गेंदा की खेती करने लगे हैं।"
सीतापुर कृषि विज्ञान केंद्र, के वैज्ञानिक डॉ दया शंकर श्रीवास्तव बताते हैं, "सरसों की घटती खेती का एक कारण गन्ना भी है, समय पर गन्ना किसानों को पर्ची नहीं मिल पाती, जिस वजह से दिसम्बर तक किसान के खेत में गन्ना रहता है। अगर दिसम्बर तक किसान के खेत में गन्ना रहेगा, तो किसान सरसों की बुवाई कब करेगा। अगर किसान नवंबर में सरसों की बुवाई करेगा तो जनवरी में माहू रोग लगने लगता है, जबकि अगर किसान अगेती सरसों की बुवाई करेगा तो जनवरी में फसल कट जाएगी।"
किसानों को सही समय पर उन्नत बीजों की अनुपलब्धता भी एक कारण है। किसानों को पता ही नहीं होता कि कौन से बीज की बुवाई करें।"पहले किसान पीली सरसों की खेती किया करता था, लेकिन अब समय के साथ उत्पादन घटने से किसान का रुझान इससे कम हो रहा है, डॉ दया शंकर ने आगे कहा।
एक समय था जब उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में सरसों के लिए प्राइवेट प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुईं थीं। बनारस का जिक्र करते हुए सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर, राजस्थान के निदेशक डॉ. पीके राय कहते हैं, "जब यूपी में सरसों का ज्यादा उत्पादन होता था तो उसकी एक वैल्यू चेन बनी हुई थी। मैं मूल रूप से बनारस का रहने वाला हूं मुझे याद है कि वहां पर सरसों प्रोसेसिंग की बड़ी यूनिट लगी हुई थी, वहां पर सरसों का तेल निकालकर पैकिंग की जाती थी। झुनझुन वाला नाम से। लेकिन उत्पादन घटने से ये यूनिट्स भी बंद हो गईं।"
लेकिन पिछले कुछ साल में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग सरसों का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के निदेशक (सांख्यिकी) डॉ. विनोद कुमार सिंह कहते हैं, "पिछले 25 साल की अगर बात करें तो सरसों का उत्पादन घटा था, लेकिन पांच साल में अभी फिर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
पिछले छह साल में उत्तर प्रदेश में सरसों का क्षेत्रफल और उत्पादन
| वर्ष | क्षेत्रफल | उत्पादन |
| 2014-15 | 5.84 लाख हेक्टेयर | 4.54 लाख मीट्रिक टन |
| 2015-16 | 5.93 लाख हेक्टेयर | 6.03 लाख मीट्रिक टन |
| 2016-17 | 6.89 लाख हेक्टेयर | 8.67 लाख मीट्रिक टन |
| 2017-18 | 6.79 लाख हेक्टेयर | 9.47 लाख मीट्रिक टन |
| 2018-19 | 7.53 लाख हेक्टेयर | 11.07 लाख मीट्रिक टन |
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में लगातार कम बारिश, कम और अनियमित बारिश और बुवाई के समय अधिक तापमान, व्हाइट रस्ट, डाउनी मिल्ड्यू और अल्टरनेटिया ब्लाइट जैसी बीमारियां, समय पर अच्छी किस्में न मिल पाना, उर्वरकों का सही प्रयोग न होना, फसल सुरक्षा के पुराने तरीके, एफिड, पेंटेड बग जैसे कीटों का प्रकोप, सरसों की देर से बुवाई, सिंचाई की सही व्यवस्था न होना भी प्रमुख कारण हैं।
देश में तोरिया, पीली सरसों, गोभी सरसों, काली सरसों की खेती होती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पश्विम बंगाल, असम, बिहार और पंजाब प्रमुख सरसों उत्पादक राज्य हैं।
देश में सरसों का क्षेत्रफल और उत्पादन
| प्रदेश | औसत उत्पादन | ||
| क्षेत्रफल (000 हेक्टेयर) | उत्पादन (000 टन) | उत्पादन (प्रति हेक्टेयर) | |
| राजस्थान | 2696.8 | 3482.2 | 1292 |
| मध्य प्रदेश | 716.9 | 813.3 | 1133 |
| उत्तर प्रदेश | 646.4 | 723 | 1114 |
| हरियाणा | 520.8 | 859.6 | 1648 |
| पश्चिम बंगाल | 452.2 | 485.2 | 1073 |
| असम | 283.9 | 183.1 | 645 |
| दूसरे राज्य | 808.3 | 833.7 | 800 |
| कुल | 6125.4 | 7380.4 | 1250 |
तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की पहल
राष्ट्रीय खाद्य मिशन के तहत तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय तेल मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एनएमईओ के तहत सरकार ने वर्ष 2024-25 तक खाद्य तेल का घरेलू उत्पादन तकरीबन 100 लाख टन से बढ़ाकर 180 लाख टन करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तिलहन फसलों का रकबा अगले पांच साल में बढ़ाकर 300 लाख हेक्टेयर से ज्यादा किया जाएगा। सरकार एक तरफ तिलहनों की उत्पादकता में 50 फीसदी वृद्धि करना चाहती है तो दूसरी तरफ खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति खपत में करीब तीन किलोग्राम की कमी करने का लक्ष्य है। देश में तिलहनों का कुल उत्पादन इस समय तकरीबन 300 लाख टन होता है जिसे अगले पांच साल में बढ़ाकर करीब 480 लाख टन करने का लक्ष्य है।
डॉ पीके राय कहते हैं, "अभी फिर से तिलहन उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा मिशन के अंर्तगत जो कार्यक्रम है तिलहन उत्पादन बढ़ाने का। इसमें पांच साल के लिए ये कार्यक्रम लांच हो रहा है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन इसे 2020 में लागू कर दिया जाएगा। दस हजार करोड़ बजट का ये कार्यक्रम पांच साल तक चलेगा। इसमें तिलहन उत्पादन पर खास जोर दिया जाएगा। इसमें सरसों के साथ ही सोयाबीन, मूंगफली का रखा है दूसरे में राइस ब्रान, पॉम, और महुआ करंज के तेल को रखा गया है। अभी नए सिरे से फिर से तेल उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इस बार तो बनारस मंडल ने सरसों उत्पादन में आगरा मंडल को पीछे कर दिया है।"
फसल सीजन 2013-14 के बाद से देश में तिलहन उत्पादन में आई कमी
देश में तिलहनों का रिकार्ड उत्पादन फसल सीजन 2013-14 में 327.49 लाख टन का हुआ था, लेकिन उसके बाद से इसमें कमी दर्ज की गई। फसल सीजन 2014-15 में तिलहन का उत्पादन घटकर 275.11 लाख टन और वर्ष 2015-16 में केवल 252.51 लाख टन का ही हुआ। फसल सीजन 2016-17 और 2017-18 में उत्पादन क्रमश: 312.76 और 314.59 लाख टन का ही हुआ। फसल सीजन 2018-19 में तिलहन का उत्पादन 322.57 लाख टन का हुआ है। तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगले पांच साल में तिलहनों का बढ़ाकर करीब 480 लाख टन करने का लक्ष्य एनएमईओ में किया गया है।
अक्टूबर से अभी तक आयातित खाद्य तेल 42 से 50 फीसदी तक हुए महंगे
देश में खाद्य तेल के कुल आयात में 65 फीसदी हिस्सेदारी पाम तेल की है। पाम तेल का आयात मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से किया जाता है, तथा इंडोनेशिया और मलेशिया में पाम तेल का उपयोग बायोडीजल में बढ़ने से आयात महंगा हो गया। घरेलू बाजार में आयातित खाद्य तेलों की कीमतों में अक्टूबर से अभी तक करीब 42 से 50 फीसदी की तेजी आ चुकी है। आरबीडी पॉमोलीन का भाव अक्टूबर में भारतीय बंदरगाह पर 567 डॉलर प्रति टन था जोकि दिसंबर अंत में बढ़कर 850 डॉलर प्रति टन हो गया। इसी तरह से क्रुड पाम तेल का भाव इस दौरान 541 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 770 डॉलर प्रति टन हो गए।
More Stories