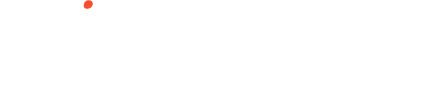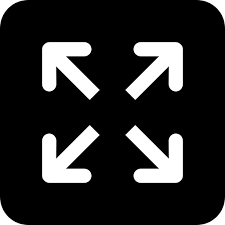पाणी नथी (पार्ट-2): बदलती जीवनशैली और 'पागल बबूल' ने कच्छ के सूखे को और भीषण बना दिया
 Ranvijay Singh 16 May 2019 11:45 AM GMT
Ranvijay Singh 16 May 2019 11:45 AM GMT
 बन्नी में पानी के तलाश में भटकते मवेशी खूब दिखते हैं। (फोटो- मिथिलेश)
बन्नी में पानी के तलाश में भटकते मवेशी खूब दिखते हैं। (फोटो- मिथिलेश)मिथिलेश धर/रणविजय सिंह
कच्छ /भुज (गुजरात)। कच्छ का बन्नी ग्रासलैंड इन दिनों भीषण सूखे की चपेट में है। ऐसा सूखा जिसमें दूर-दूर तक सिर्फ धूल ही धूल नजर आती है। कहा जा रहा है कि पिछले 20 सालों का ये सबसे भीषण सूखा है। कच्छ या बन्नी के लिए सूखा नई बात नहीं है लेकिन इस साल की विभीषिका के लिए मालधारियों की बदलती जीवनशैली और ग्रासलैंड में फैले गांडो बावर (पागल बबूल) को प्रमुख जिम्मेदार बताया जा रहा है।
बन्नी के क्षेत्र में आपकी नजर जहां तक पहुंचेगी वहां तक आपको बस सूखा ही दिखेगी। लेकिन इस नजारे के उलट ग्रासलैंड के होड़को के सेठरीपुर गांव में एक जगह ऐसी भी है जो हरी भरी दिखती है। यह जगह गांव के ही रहने वाले युसुफ हालीपोतरा (70 साल) की है। युसुफ दिन की गर्मी में अपनी इस"> हरी भरी जगह (विरड़ा) में बैठकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ''उनके पास बहुत मीठा पानी है, वो इस भीषण सूखे को झेल जाएंगे।''
एरिड एरिया (शुष्क क्षेत्र) होने के कच्छ में सूखा पड़ना आम बात है। ऐसे में ग्रासलैंड में रहने वाले मालधारी (पशुपालक) सूखे से निपटने के लिए झील और विरड़ा (रेन वॉटर हार्वेसटिंग सिस्टम) बनाया करते हैं।
युसुफ भी उन चुनिंदा मालधारियों में से हैं जिन्होंने विरड़ा बनाया था और अब उसी की बदौलत सूखे से निपटने की बात कहते हैं। युसुफ अपने हरे भरे विरड़ा में बैठकर कहते हैं, ''मैं अपने बचाए हुए पानी से दो महीने गुजार दूंगा। इससे मेरे परिवार और माल (पशु) को पानी मिल जाएगा।''
बन्नी ग्रासलैंड कुल 2,500 स्क्वायर किमी में फैला हुआ है। कच्छ का यह तालुका देश के कई बड़े जिलों से भी बड़ा है, जबकि पूरा जिला 45,000 स्क्वायर किमी में फैला हुआ है। इस पूरे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार का घास पाई जाती है। यहां की आबादी पूरी तरह से मवेशियों पर निर्भर रहती है।
ऐसी क्या वजह रही कि युसुफ इस सूखे को झेलने की तैयारी कर पाए जबकि ग्रासलैंड में रहने वाले ज्यादातर मालधारी सूखे की वजह से पलायन करने को मजबूर हो गये। इसका जवाब बन्नी ग्रासलैंड में काम करने वाली संस्था सहजीवन के कार्यकारी निदेशक डॉ. पंकज जोशी देते हैं।
पंकज कहते हैं, ''ग्रासलैंड में रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल में आया बदलावा इसका प्रमुख कारण है।'' सहजीवन संस्था कच्छ में पिछले 35 साल से पानी और पारिस्थितिकी तंत्र (इको सिस्टम) पर काम कर रही है।
पंकज आगे कहते हैं, ''ग्रासलैंड में पशुओं की संख्या इंसानों के मुकाबले हमेशा ज्यादा रही है। ऐसे में सूखे का सबसे ज्यादा असर भी पशुओं पर ही पड़ता है। पहले ग्रासलैंड में रहने वाले मालधारी सूखे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो पशुओं की संख्या कम रखते थे जिससे सिर्फ उनका भरण पोषण हो सके। साथ ही झील और विरड़ा विधि के माध्यम से बारसत में पानी को जमीन में संचित करते थे, और यही पानी सूखे के समय में उनके और मवेशियों के काम आता था।"
कच्छ से सूखे पर फेसबुक लाइव
''सन 2000 के बाद स्थिति में तेजी से बदलाव आया। कच्छ में औसत बारिश (320 एमएम) से ज्यादा बारिश होने लगी। ऐसे में लोग ग्रासलैंड में ही गैरकानूनी तौर पर खेती करने लगे। 2001 में आए भूकंप के बाद तेजी से सड़कों का निर्माण हुआ। इसकी वजह से पास के शहर कच्छ तक मालधारियों की पहुंच आसान हो चली। इसी बीच मिल्क इकॉनोमी ने ग्रासलैंड में दस्तक दी। ऐसे में जो मालधारी पहले अपने भरण पोषण के लिए पशुओं को रखते थे अब उन्हें दूध के कारोबार के लिए रखने लगे। एक-एक मालधारी के पास 100 से 150 गाय-भैंस रहती हैं। जीवनशैली में आए इस बदलाव की वजह से मालधारी इसबार आए सूखे को झेल नहीं पाए।'' पंकज जोशी कहते हैं।
वर्ष 2012 में जब पशु जनगणना हुई थी तब कच्छ में कुल 19 लाख मवेशी थे, ये जिले की आबादी 20 लाख के लगभग के बराबर है। इन मवेशियों में भैंस, गाय, बकरी और ऊंट हैं। ऊंटों की संख्या 10 लाख के आसपास बताई गयी थी। ये प्रदेश कुल मवेशियों का लगभग 5.75 फीसदी हिस्सा है।
पंकज जोशी की बात से एरिड कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉ. योगेश जडेजा भी सहमति जताते हैं। वो कहते हैं, ''यह सही बात है कि मालधारियों की जीवनशैली में आया बदलाव बहुत बड़ा कारण है कि वो इस सूखे से परेशान हैं। बन्नी ग्रासलैंड ऐसी जगह नहीं है जहां सामान्य जीवन जिया जा सके। इसी वजह से मालधारी पहले सूखे के लिए तैयार रहते थे, लेकिन सन 2000 के बाद वो अपनी इस तैयार रहने की आदत को भूलते गए। इसके पीछे बरसात के पैटर्न में आया बदलाव, वॉटर पॉलिटिक्स और पाइप लाइन से पानी देने जैसी वजह हैं।''
डॉ. योगेश जडेजा आगे कहते हैं, ''वॉटर पॉलिटिक्स की वजह से इलाके में पाइप लाइन से पानी पहुंचने लगा। ऐसे में यहां रहने वाले ज्यादातर मालधारियों ने अपनी पारंपरिक झील और विरड़ा विधि का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और सप्लाई के पानी पर निर्भर हो गए। अब सन 2000 के बाद लगातार हो रही अच्छी बरसात का पैटर्न 2018 में टूट गया। 2018 में सिर्फ 28 जून को बारिश हुई और इसके बाद बारिश नहीं हुई, जिस वजह से 2019 में भारी सूखा पड़ा है। और क्योंकि ज्यादातर मालधारी अपने पारंपरिक रहन सहन को भुला चुके हैं, ऐसे में उन्हें इस सूखे की मार ज्यादा पड़ी है।''
गुजरात सरकार ने 13 दिसंबर 2018 में कच्छ को सूखा घोषित किया था, जोकि अभी भी कायम है। सूखा घोषित होने के बाद से ही सरकार की ओर से बन्नी ग्रासलैंड के इलाके में कैटल कैंप चलाए जा रहे हैं, जहां पशुओं को चारा दिया जाता है।
भुज के डिप्टी मामलातदार मोहित सिंह बताते हैं, ''आठ मई तक के आंकड़ों के मुताबिक अभी 481 कैटल कैंप चलाए जा रहे हैं। इनमें 284983 को चारा दिया जा रहा है।''
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के 401 एक गाँव सूखे की चपेट में हैं। इनमें से 50 फीसदी या अधिक फसलों के नुकसान वाले गाँवों की सबसे ज्यादा संख्या कच्छ जिले की है।
स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के आंकड़ों की मानें तो वर्ष 2018 में कच्छ में औसतन जितनी बारिश होनी चाहिए थी उसका 25 फीसदी ही हुई है। आईएमडी के अनुसार, कच्छ में 2017 में औसत वर्षा में 56.58 फीसदी की कमी थी। कच्छ में 320 एमएम (मिली मीटर) औसत बारिश मानी गई है।
ग्रासलैंड में चारे के लिए अलग से कैंप खुलने से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने बदतर हैं। अगर आंखों देखी बात कही जाए तो इलाके में दूर-दूर तक सिर्फ सूखी हुई जमीन और उस पर उगे प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा (Prosopis juliflora, विलायती बबूल) के पेड़ नजर आते हैं।
प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा को यहां के लोग 'गांडो बावर' कहकर पुकारते हैं यानि 'पागल बबूल'। स्थानीय लोग सूखे के लिए इस पेड़ को भी जिम्मेदार मानते हैं।
होड़को के रहने वाले हाबू भाई (40 साल) बताते हैं, ''इस पेड़ को गांडो बावर इस लिए कहते हैं क्योंकि यह पागलों की तरह इलाके में फैल रहा है। इसकी जड़ें जमीन में फैली होती हैं और यह जमीन से पानी का बहुत दोहन करता है।'' हाबू भाई पास ही के एक देसी बबूल के पेड़ को दिखाते हुए कहते हैं, ''पहले इलाके में देसी बबूल बहुत होते थे, लेकिन जबसे गांडो बावर आया उसने सब सुखा दिया।''
अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलोजी एंड एनवायरमेंट बेंगलुरू से रिसर्च स्कॉलर रम्या रवि ने बन्नी ग्रासलैंड में प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा को लेकर रिसर्च किया है। वो बताती हैं, ''बन्नी में 1960 में प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा लाया गया। इसके पीछे कई वजह थीं। सबसे बड़ी वजह थी कि बन्नी ग्रासलैंड तेजी से बंजर हो रहा था। वैसे तो यह इलाका ग्रासलैंड का है, लेकिन यहां सूखा भी बहुत पड़ता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 1901 से 1990 के बीच ही करीब करीब 57 बार सूखा पड़ा है। ऐसी स्थिति में बन्नी से सटे हुए रण की वजह से यह इलाका भी बंजर होने की कगार पर था। इसे रोकने के लिए वन विभाग की ओर से प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा यहां लगाया गया।''
रम्या रवि कहती हैं, ''1980 तक यह समस्या नहीं था, लेकिन 1980 के बाद यह समस्या बनता गया। लोग इसे एक गांव से दूसरे गांव में लगाने लगे थे। पशु इसका फल खाते और उनके मल से भी इसका फैलाव होता। बारिश की वजह से यह तेजी से बढ़ा और फिर इतना फैल गया कि पशुओं के लिए ही दिक्कत होने लगी। साथ ही इसका फल (प्रोसोपिस पॉड) गाय और भेड़ के लिए नुकसानदायक भी है। वो इसे पचा नहीं पाते।'' रम्या रवि बताती हैं, ''बन्नी के करीब 70 प्रतिशत इलाके में अभी गांडो बावर का कब्जा है। ऐसे में यह समस्या तो है ही। जो ग्रासलैंड है वो वुड लैंड में बदलता जा रहा है। अब जो इलाका पहले से सूखा है वहां इसका होना और खराब है।''
बन्नी में फैले गांडो बावर की लकड़ियों का यहां के लोग उपयोग भी कर रहे हैं। इसकी लकड़ी से खुद के और जानवरों के रहने के लिए शेड बनाए जाते हैं। साथ ही लोग इससे चारकोल भी बना रहे हैं। हालांकि इन सब मुनाफे के बाद भी सूखे से त्रस्त लोग इसे बेकार और पागल ही करार देते हैं। होड़को के सेठरीपुर गांव के युसुफ हालीपोतरा भी अपने विरड़ा में बचे पानी के पीछे आस पास के इलाके में गांडो बावर का न होना बताते हैं। युसुफ कहते हैं, ''मैंने विरड़ा के आस पास से गांडो बावर के सभी पेड़ हटा दिए। इसकी वजह से ही मेरा पानी बच पाया है। गांडो बावर होता तो सबपानी पी जाता।''
यह भी पढ़ें- पाणी नथी: 'इस गांव में मैं अकेला शख्स बचा हूं, गांव के सभी लोग यहां से चले गए'
कच्छ से फेसबुक लाइव
More Stories