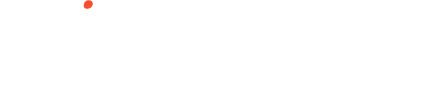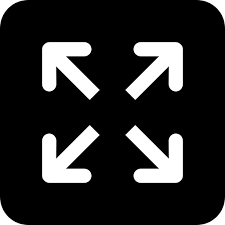देश के 70 फीसदी छात्र बारहवीं के आगे नहीं पढ़ पाते, लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं है
लोकतंत्र में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों में रोटी, कपड़ा और मकान के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य को रखा जाता है। लेकिन लोकतंत्र के महान पर्व 'लोकसभा चुनाव 2019' में यह मूलभूत मुद्दे कहीं गायब हैं। गांव कनेक्शन की कोशिश है कि आम चुनाव से पहले इन मुद्दों और उनके वास्तविक स्थिति से लोगों को परिचित कराया जाए। किसानों की स्थिति, स्वास्थ्य, पर्यावरण के बाद गांव कनेक्शन की इस विशेष सीरिज 'इलेक्शन कलेक्शन' में आज शिक्षा का मुद्दा।
 Daya Sagar 10 April 2019 12:45 PM GMT
Daya Sagar 10 April 2019 12:45 PM GMT

लखनऊ। सीमा (15) प्राथमिक विधालय, बयारा, संत कबीर नगर (उत्तर प्रदेश) में आठवीं कक्षा की छात्रा है। उसके घर से उसका स्कूल 3 किलोमीटर दूर है इसलिए वह साइकिल से स्कूल आती है। उसे अब गांव की संकरी पगडंडियों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाने में डर नहीं लगता। हालांकि लड़की होने की वजह से सीमा के घर वाले जरूर डरते हैं।
सीमा आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। लेकिन उसे नहीं पता कि वह आगे अपनी पढ़ाई जारी रख पाएगी या नहीं? वजह, एक लड़की होने की वजह से घर वाले आगे की शिक्षा के लिए उसे अधिक दूर नहीं भेज सकते और उसके घर से निकटतम इंटर कालेज की दूरी पांच किलोमीटर है।
सीमा की तरह ऐसी कई लड़कियां हैं जो मन होते हुए भी आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती। असर (Annual Status of Education Report) की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 18 साल की आयुवर्ग की लड़कियों में 13.5 प्रतिशत लड़कियों का नामांकन ऊपर की कक्षाओं में नहीं हो पाता है। कई लड़कियों का नामांकन तो हो जाता है लेकिन उनकी उपस्थिति का रिकॉर्ड काफी खराब रहता है।
ऐसा नहीं है कि असर की रिपोर्ट का यह ट्रेंड सिर्फ लड़कियों के लिए है। लड़कों की ड्रॉप आउट (आठवीं या बारहवीं के बाद स्कूल छोड़ देना) संख्या में भी कुछ खास सुधार नहीं आया है। शिक्षा का अधिकार (RTE-2009) और अनिवार्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा लागू होने के बावजूद पिछले दस साल में असर के आंकड़े उत्साहवर्धक नहीं है। शिक्षा में नामांकन दर बढ़कर 96% अवश्य हो गई है, लेकिन आज भी 20% बच्चे प्राथमिक शिक्षा और 36% बच्चे उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। वहीं देश के लगभग 70 प्रतिशत विद्यार्थी 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं।
उच्च शिक्षा का भी यही हाल है। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविधालयों की रैंकिंग में विश्व के शीर्ष सौ विश्वविधालयों में देश का एक भी विश्वविधालय नहीं है। वहीं देश में शिक्षकों की हालत भी खासा खराब है। एक रिपोर्ट की माने तो इस समय देश में शिक्षकों के लगभग 5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। शिक्षकों की यह पूर्ति एडहॉक शिक्षकों और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों के द्वारा पूरी की जाती है। इन एडहॉक शिक्षकों और शिक्षामित्रों की भी हालत कुछ खास उत्साहजनक नहीं है और आए दिन ये एडहॉक शिक्षक और शिक्षामित्र अपने अधिकारों और मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं।
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और शिक्षाविद् डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, "शिक्षा अधिकारों को प्राप्त करने का प्रथम साधन होता है और इसकी सहायता से आम लोग प्रशिक्षित होकर लोकतंत्र में 'नागरिक' बनते हैं।" अमेरिका के महान शिक्षाविद् होराक मैन ने भी कहा था, "शिक्षा नागरिकों का एकमात्र राजनीतिक साधन है, जिसकी नांव पर सवार होकर लोकतंत्र की नदी में उतरा जा सकता है। शिक्षा के बिना यह नाव कहीं भी डूब सकती है।"
इन शिक्षाविदों के कथन से साफ पता चलता है कि लोकतंत्र में शिक्षा का अपना महत्व है। हालांकि लोकतंत्र के महान पर्व यानी कि चुनावों में कभी भी यह प्रमुख मुद्दा नहीं बन पाता है। आज भी देश के प्रमुख राजनीतिक दल जाति, धर्म, मंदिर, सेना और पाकिस्तान पर राजनीति करते हैं। इनकी चुनावी सभाओं में इन सभी मुद्दों के अलावा अधिक से अधिक बेरोजगारी और विकास (आर्थिक विकास) का मुद्दा ही शामिल हो पाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मुद्दे अभी भी राजनीतिक दलों के लिए कुछ खास मायने नहीं रखते।
महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविधालय, चित्रकूट (मध्य प्रदेश) में प्रोफेसर जयशंकर मिश्रा कहते हैं, "भारतीय परिदृश्य में राजनीतिक दल चाहते ही नहीं हैं कि उनके सामने कोई सवाल खड़ा करने वाला एक समूह खड़ा हो, इसलिए वह शिक्षा को चुनावी मुद्दा कभी बनाते ही नहीं हैं।" जयशंकर मिश्रा मानते हैं कि भारत में शिक्षा की हालत बहुत खराब है, फिर चाहे वह उच्च शिक्षा हो या प्राथमिक शिक्षा। लेकिन उन्हें अपने पचास साल के करियर में याद नहीं कि कब किसी नेता या पार्टी ने सार्वजनिक मंच से शिक्षा के लिए बात की हो।
शिक्षा को लेकर राजनीतिक दलों की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इनके घोषणा पत्रों में शिक्षा की बात महज एक पन्ने में सिमट कर रह जाती है। दो विपरीत ध्रुवों वाली राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में भी शिक्षा के लिए लगभग एक समान और परंपरागत रूप से पुरानी हो चुकी बातें लिखी जाती हैं।
अंबेडकर विश्वविधालय में मीडिया स्टडीज के शोध छात्र अनुराग अनंत इसकी ऐतिहासिकता के बारे में हमारा ध्यान दिलाते हैं। अनुराग कहते हैं, "नेहरू और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद शिक्षा के क्षेत्र में किसी ने ध्यान नहीं दिया और फिर अस्सी के दशक तक आते-आते हमारे देश की राजनीति जाति और धर्म आधारित हो गई। राजनेताओं ने पहले जनता को जाति और धर्म आधारित मुद्दों पर भटकाया। धीरे-धीरे जनता को इसकी आदत हो गई। अब जनता खुद नहीं चाहती कि शिक्षा जैसे अहम मसले पर बात हो।"
अनुराग आगे कहते हैं कि पहले शिक्षा का सीधा संबंध रोजगार से होता था। लेकिन अब इस की कोई गारंटी नहीं कि शिक्षा मिलने के बाद आपको रोजगार मिले। इसलिए भी लोग शिक्षा के प्रति धीरे-धीरे उदासीन होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "भारत में शिक्षा भले ही एक चुनावी मुद्दा ना हो लेकिन विदेशों में शिक्षा को लेकर चुनाव लड़े जाते रहे हैं।"
पढ़ें- इस चुनाव में गन्ने का कसैलापन कौन चखेगा ?
नहीं लागू हो पाई नई शिक्षा नीति
शिक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नई शिक्षा नीति के लिए पिछले पांच साल में दो समितियां गठित हुई लेकिन नई शिक्षा नीति लागू नहीं हो सकी। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने 2014 के घोषणा पत्र में नई शिक्षा नीति बनाकर उसे लागू करने का वादा किया था। इससे पहले शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई थी। आदर्श रूप में शिक्षा नीति को हर 20 साल पर मूल्यांकन कर इसमें परिवर्तन लाना रहता है लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा कभी नहीं हो सका।
देश की शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण, शिक्षा नीति से ही होता है। इस शिक्षा नीति के निर्धारण के लिए आयोगों का गठन होता है। देश के आजादी के बाद पहली बार 1948 में विश्वविद्यालयी शिक्षा को दुरूस्त करने के लिए 'राधाकृष्णन आयोग' का गठन हूआ था। इस आयोग के अध्यक्ष देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और प्रमुख शिक्षाविद डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से 1952 में मुदालियार आयोग का गठन हुआ।
स्कूली शिक्षा को ध्यान में रखते हुए 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया। कोठारी आयोग के सुझावों को ध्यान में रखते हुए ही देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में बनी। कोठारी आयोग का सबसे प्रमुख सुझाव था कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का छः प्रतिशत शिक्षा के मद में खर्च किया जाए।
प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में इसे एक राष्ट्रीय लक्ष्य भी बनाया गया। लेकिन इस राष्ट्रीय लक्ष्य को आज 40 साल बाद भी नहीं प्राप्त किया जा सका है। 1968 की राष्ट्रीय नीति के बाद 1986 के दूसरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस लक्ष्य को दोहराया गया।
1992 की यशपाल समिति, 2016 के टीआरएस सुब्रमण्यन समिति और भारत सरकार की प्रमुख नीति नियंता 'नीति आयोग' भी लगातार 6 प्रतिशत खर्च करने की अनुशंसा करती रही है। नीति आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट 'स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया 75' में कहा है कि 2022 तक भारत सरकार को शिक्षा पर खर्च को वर्तमान से दोगुना करते हुए जीडीपी का न्यूनतम 6 प्रतिशत सुनिश्चित करना चाहिए।
सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले पांच सालों में शिक्षा पर जीडीपी का खर्च औसतन 2.5 प्रतिशत से 2.8 प्रतिशत रहा, जो कि निर्धारित लक्ष्य का आधा भी नहीं है। ऐसा निकट भविष्य में भी संभव होता नहीं दिख रहा है! शिक्षा के मद में खर्च का सीधा संबंध शिक्षा की गुणवत्ता से होता है।
अगर हम वैश्विक आंकड़ों की बात करें तो वैश्विक आंकड़ें भारत से कहीं बेहतर हैं। शिक्षा पर खर्च का वैश्विक औसत जीडीपी का 4.7 प्रतिशत है। अमेरिका अपनी जीडीपी का 5.6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है। जबकि नार्वे और क्यूबा जैसे छोटे देश अपनी जीडीपी का क्रमशः 7 और 13 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करते हैं। भारत के समान अर्थव्यवस्था वाले देश ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका दोनों शिक्षा पर लगभग अपनी जीडीपी का 6 प्रतिशत खर्च करते हैं।
कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में शिक्षा पर जीडीपी के न्यूनतम 6 प्रतिशत खर्च करने की बात कही है। जबकि सत्तासीन बीजेपी के घोषणा पत्र के शिक्षा कॉलम में यह नदारद है। इससे पार्टियों और सरकारों का राष्ट्रीय शिक्षा लक्ष्य के प्रति गंभीरता का पता लगाया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास आरंग में ग्रामीण गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाने वाली गिरीजा शुक्ला (60) कहती हैं, "शिक्षा के महत्व को सभी जानते हैं लेकिन इस पर बात करने वाला कोई नहीं है। मैंने अपने 40 साल के करियर में कभी किसी भी नेता को शिक्षा के बारे में बात करते नहीं सुना।" वह इसके लिए मीडिया को भी दोषी मानती हैं कि मीडिया कभी भी शिक्षा के मुद्दे को खासकर चुनावों के समय कभी गंभीरता से नहीं उठाती है।
प्याज की राजनीति- 'किसानों के आंसुओं में वो दम नहीं कि सरकार हिला सके'
आधुनिक भारत के प्रमुख शिक्षाविद् और पूर्व एनसीईआरटी प्रमुख प्रोफेसर कृष्ण कुमार का मानना है कि अगर आप देश में शिक्षा के स्तर को लेकर चिंतित हैं और इसमें सुधार देखना चाहते हैं, तो इसे राजनीति से जोड़कर ही देखना होगा। वह शिक्षा को राजनीति से जोड़ने और इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की बात कहते हैं। वह अपनी पुस्तक, 'राज, समाज और शिक्षा' में लिखते हैं, "आज की जरूरत है कि हम शिक्षा का राजनीतिक संदर्भ पहचाने और राजनीति की पुनर्रचना में शिक्षा का संदर्भ तय करें।"
शिक्षा पर काम करने वाले एक स्वंयसेवी कार्यकर्ता ने नाम ना बताने की शर्त पर गांव कनेक्शन से अपनी बातें साझा की। उन्होंने कहा, "शिक्षा चुनावी मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि यह कोई तात्कालिक परिणाम नहीं दे सकता। अगर शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसके परिणाम 10-20 साल बाद ही देखने को मिलेंगे। जबकि चुनावी दल कोई ऐसा मुद्दा खोजते हैं जो कि उन्हें तात्कालिक लाभ दे।"
वह आगे कहते हैं, "किसी भी व्यवस्था में परिवर्तन नेताओं और नौकरशाहों की इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। चुंकि नेताओं और नौकरशाहों के संतान सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते तो वे भी इस पर अधिक ध्यान नहीं देते। देश का मिडिल क्लास के लिए भी यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि वह भी अपने बच्चों को पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूलों में भेजता है। जबकि देश की गरीब जनता के लिए रात की रोटी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके लिए अभी रोटी के ही लाले है और वह दिन भर इसी जुगत में रहता है कि रात में परिवार को रोटी कैसे मिलेगा। इसलिए वह शिक्षा जैसे मुद्दों पर कभी नहीं बोलता।"
उन्होंने सुझाया कि अगर इच्छाशक्ति हो तो इस व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। वह सरकारी अस्पतालों का उदाहरण देते हैं कि सरकारी अस्पतालों की हालत अब सुधरी है क्योंकि मिडिल क्लास अब सरकारी अस्पतालों में जाने लगा है। वह कहते हैं कि इसी तरह सरकारी शिक्षा में भी सुधार लाया जा सकता है, बशर्ते नेता, नौकरशाह और मिडिल क्लास इसमें रूचि दिखाएं।
More Stories