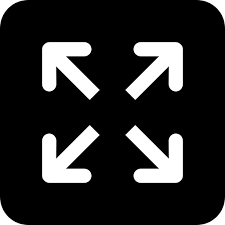'सुपर-वुमन का तो पता नहीं मगर पोस्ट-वुमन ज़रूर होती हैं'
कई बार जब लोगों के घर जाती हूँ तो पहले उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगता है कि मैं डाकिया हूँ। लेकिन बहुत ख़ुशी होती है जब वह मेरे बारे में जान ना चाहते हैं और अपने घर के लोगों को भी बताते हैं, 'देखो, महिला डाकिया भी होती हैं, हमें तो पता ही नहीं था!'
 Jigyasa Mishra 10 Oct 2018 3:32 AM GMT
Jigyasa Mishra 10 Oct 2018 3:32 AM GMT

लखनऊ: यूँ तो डाकघर खुलने का समय 10 बजे होता है लेकिन चिट्ठी बाँटने निकलने से पहले की तैयारी के लिए डाकिये, सुबह 8:30 बजे से ही डाकघर में मौजूद हैं। 9:30 बज चुके हैं और डाकघर का वह बड़ा सा कमरा जिसमें डाकिये अपनी डाकें छांट रहे हैं, खचाखच भरा हुआ है। सरकारी दफ़्तर के इसी कमरे के एक डेस्क पर डाकिओं जैसी ही, खाकी वर्दी में बैठी एक महिला डाकों को छांटने में लीन है।
खाकी सलवार-कमीज़ और शरीर के ऊपरी हिस्से में दुपट्टे को कंधों पर खींच कर अंग्रेज़ी अक्षर का वी (V) बनाये हुए, डाकों की दो गठरी बना कर बाजू में रखते हुए, साजदा तीसरी गठरी के लिए चिट्ठियां छांटने लगती है।
लखनऊ के गोमतीनगर (विभूती खण्ड) में स्थित पोस्ट आफिस में कुल 35 डाकियों में साजदा बानो इकलौती महिला हैं।
यह भी पढ़ें: डाकिया डाक लाया: भावनाओं को मंज़िल तक पहुँचाती चिट्ठियां
"हमारे यहाँ अकेली महिला डाकिया हैं ये पर किसी पुरुष से काम नहीं। हमेशा वक़्त से पहले पहुचती हैं और सभी पुरुष डाकियों कि ही तरह साइकिल से हर घर डाक पहुचाती हैं। कभी किसी बिल्डिंग में लिफ्ट न चलने पर ये 8 माले ऊपर तक पैदल पहुँच कर भी चिठ्ठी पहुँचाती हैं," गोमतीनगर के पोस्ट मास्टर नीलेश श्रीवास्तव बताते हैं।
साजदा के पति के देहांत के बाद उसे जब डाकिये की नौकरी मिली थी तो उसके लिए वह एक मुश्किल निर्णय था। जिसने पहले कभी रसोई के बाहर कदम नही रखा था उसके लिए बग़ैर मौसम की फ़िकर किए, गलियों में जाकर डाक बाँटना किसी चुनौती से कम नहीं था। "हमारे पति के गुज़रने के बाद जब हमको डाकिये की नौकरी मिली तो हमने सोचा कि ये तो मर्दों का काम है, बहुत मेहनत लगती है, हम नही कर पाएंगे। लेकिन उसी दिन हमने एक महिला लेबर को खोपड़ी (माथे) पर ईंट ढ़ोते देखा और उसी वक़्त निर्णय लिया कि यदि ये काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं!," पुरानी यादें ताज़ा करके साजदा के चेहरे पर एक सूकून भरी मुस्कान साफ़ दिखती है।
साजदा बताती हैं-
मजबूरी अब स्वाभिमान बन गई: डाकिये का काम शुरू तो हमने मजबूरी में किया था, घर परिवार का खर्चा उठाना था, वरना हमलोग खाते क्या! लेकिन अब तो कुछ औऱ ही बात है। हमें लगता है यह हमारी ज़िंदगी का सबसे सही और बेहतरीन फैसला है। हमें किसी के भी आगे हाथ फैलाने या मदद माँगने की ज़रूरत नहीं। जितना कमाते हैं, अपनी मेहनत का कमाते हैं।
बहुत मिलता है सम्मान: कई बार जब लोगों के घर जाती हूँ तो पहले उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगता है कि मैं डाकिया हूँ। उनकी ग़लती नही है, ऐसे कई पेशे हैं जिसमें लड़कियां कभी दिखती ही नहीं तो लोग तो वैसे ही सोचेंगे। लेकिन बहुत ख़ुशी होती है जब वह मेरे बारे में जान ना चाहते हैं और अपने घर के लोगों को भी बताते हैं, 'देखो, महिला डाकिया भी होती हैं, हमें तो पता ही नहीं था!'
'पोस्ट-वुमन' एक अलग ही खुशी देता है: एक दफ़ा जब चिट्ठी देने एक घर गए तो करीबन 5-6 साल का एक बच्चे ने अपने दरवाज़े पर मुझे देखते ही अंदर आवाज़ दी, 'मम्मी, पोस्ट-वुमन आयी है!' उसकी माँ ने मुझसे अपना डाक लेते हुए कहा, "इतनी धूप में भी आप आई हैं, किसी सुपर-वुमन से कम काम नहीं है आपका!" वो बहुत ही गर्व भरा वक़्त था मेरे लिए क्यों कि इस से पहले मैंने कभी ये शब्द सुना ही नही था। सब पोस्ट-मैन ही बोलते हैं, फ़िर चाहे आप महिला ही क्यों न हों। तब गौर किया मैंने कि सुपर-वुमन का तो पता नहीं मगर पोस्ट-वुमन ज़रूर होती हैं।
More Stories