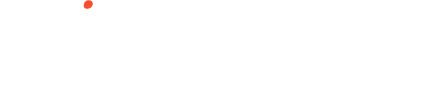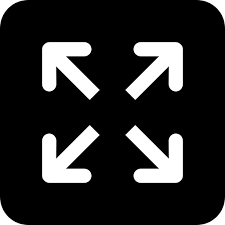संवाद: भारत के कृषि वैज्ञानिकों का ज्ञानोदय रिटायरमेंट के बाद ही क्यों होता है?
 गाँव कनेक्शन 2 Oct 2016 12:07 PM GMT
गाँव कनेक्शन 2 Oct 2016 12:07 PM GMT
 भारतीय कृषि शोध की दुर्दशा वैज्ञानिकों के अहंकार ने की है: रमनजनैयुलु जीवी
भारतीय कृषि शोध की दुर्दशा वैज्ञानिकों के अहंकार ने की है: रमनजनैयुलु जीवीरमनजनैयुलु जीवी
उदासीनता, निहित स्वार्थ, अति अहंकार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव और सामाजिक आर्थिक/पारिस्थितिकि चिंताओं को नज़रअंदाज करते रहने जैसे कारणों ने कृषि के शोध तंत्र को बर्बाद कर दिया है। जब भी शोध तंत्र से संबंधित किसी मुद्दे पर सवाल उठते हैं तो या तो सिस्टम के लोग इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने की मजबूरी गिनाने लगते हैं या फिर ये कह देते हैं कि जो उन्हें समझ न आए, वो विज्ञान नहीं।
'सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर' (सीएसए) को स्थापित करने के पीछे के प्रमुख कारणों में से एक था किसानी के तमाम उपयोगी तरीकों को वैज्ञानिक नज़रिए से समझना फिर बाद में उसे मुनाफे के लिए विस्तार देना। इस केंद्र को स्थापित करने के दौरान हम बहुत से उच्चाधिकारियों से मिले ये समझने के लिए कि कौन सी तकनीकें फायदेमंद हैं, लेकिन हमारे ये प्रयास हमेशा विफल रहे। ऐसे ही कुछ अनुभव आपको बताता हूं।
बिना कीटनाशक के खेती करने की एनपीएम तकनीक का जब हमने सफलतापूर्वक कई गाँवों में परीक्षण कर लिया तो हमने कुरनूल ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और विस्तार अधिकारियों को तकनीक को परखने के लिए फील्ड विज़िट पर बुलाया। जितने भी वैज्ञानिक फील्ड विज़िट पर आए थे उन्हें तकनीक बेहद पसंद आई पर फिर भी इसे आगे बढ़ाने के लिए कृषि विस्तार के निदेशक ने इंकार कर दिया। तकनीक को आगे बढ़ाने का कारण ये दिया कि इसे उनके वैज्ञानिकों ने विकसित नहीं किया है न ही परीक्षण किया है। मैंने ये तर्क दिया कि विश्वविद्यालय बहुत से ऐसे कीटनाशक प्रमोट करता है जिसे उसके वैज्ञानिकों ने ना ही बनाया, ना ही उसका परीक्षण किया और ये भी कहा कि आप नई तकनीक पर शोध शुरू कर दीजिए। लेकिन वो निदेशक नहीं माने।
कुछ समय बाद इसी मुद्दे को लेकर हम कृषि विश्वविद्यालय के शोध विभाग के निदेशक से भी मिले। हमने उनसे कहा कि आप हमारी विकसित एनपीएम तकनीक पर कृपया शोध करें और हमें बताएं कि इस तकनीक में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं?इसके बाद कई सालों तक हम उनसे पूछते रहे कि शोध का क्या हुआ और वो हमेशा हमें यही जवाब देते उन्होंने शोध केंद्रों को लिखा है पर कोई इस पर शोध करने को तैयार नहीं। आगे चलकर वो अधिकारी उसी कृषि विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बन गये। हम उनसे फिर कई बार मिले पर कुछ नहीं हुआ।
साल 2007 में वर्ल्ड बैंक संस्था के एक वरिष्ठ अधिकारी इच्छुक थे कि वे एक आईटी तकनीक के इस्तेमाल से एक ऐसा ढांचा तैयार कर सकें जो किसानों की मदद कर सके। हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान में इस विषय पर मेरी उन सज्जन से मुलाकात हुई। मैंने अपना मत रखते हुए कहा कि यह तकनीक ज्ञान आधारित होनी चाहिए, जिससे किसानों को खेती के कई सफल उदाहरणों की जानकारी मिले, उसमें सिर्फ ये न बताया जाए कि विश्वविद्यालय के किसानों को क्या सुझाव हैं। किसानों को कौन सी तकनीक और कौन सा उदाहरण अपनाना है ये चुनाव उन पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। उसी कृषि विस्तार निदेशक ने फिर से हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया।
इस सब से उक्ता कर 2010 के बाद हमने कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ बात करना, उनका पीछा करना छोड़ दिया। हमने सोचा कि हम वही करेंगे जो करते आए हैं, अपने तरीके से ही किसानों तक पहुंचेंगे।
साल 2013 में एक दिन अचानक फिर मेरी मुलाकात उन्हीं कृषि विस्तार के निदेशक से हुई जिन्होंने खेती को रसायन से बचाने की हमारी सभी तकनीकों को ठुकराया था, अब वो रिटायर हो चुके थे और रसायन मुक्त मिर्च की खेती को प्रमोट कर रहे थे। अब वो प्राकृतिक खेती, रसायन रहित खेती का ज़ोरों-शोरों से प्रमोशन करते हैं।
वैज्ञानिकों के सारे ज्ञान का उदय उनके रिटायरमेंट के बाद ही क्यों होता है?जयराम रमेश, पूर्व पर्यावरण मंत्री
वो अधिकारी जिसने हमारे लगभग पीछे पड़ जाने के बावजूद वैकल्पिक खेती और रसायन मुक्त खेती की तकनीकों में कोई रूझान नहीं दिखाया, अब खुद रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक संस्थान चला रहा है।
मुझे याद है जब जयराम रमेश ने बीटी-बैंगन पर सलाह-मशविरे के दौरान हैदाबाद में क्या कहा था। एक तरफ किसान बीटी-बैंगन की खेती के व्यवसायिकरण का विरोध कर रहे थे और एनजीओ पर्यावरण की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार, अतिरिक्त विकल्पों को लेकर मुद्दा उठा रहे थे, कृषि विश्वविद्यालय और केंद्रों के वैज्ञानिक इसे लागू करने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि ये तो एक वैज्ञानिक बढ़ोतरी है और इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन इसी दौरान कुछ रिटायर्ड वैज्ञानिक कह रहे थे कि हमें सचेत रहना चाहिए, अपनी मौजूदा तकनीकों को खत्म नहीं करना चाहिए जब तक बीटी तकनीक के बारे में जैव-सुरक्षा का सबूत न मिल जाए तब तक इस पर रोक लगा देनी चाहिए। जयराम रमेश ने कहा था कि वैज्ञानिकों के सारे ज्ञान का उदय उनके रिटायरमेंट के बाद ही क्यों होता है?
वो समय आ गया है जब कृषि वैज्ञानिकों को ये समझना होगा कि विज्ञान चाहरदीवारी में उनके द्वारा किए जा रहे प्रयोग से ज्यादा विस्तृत है। उन्हें अपनी सोच का दायरा बड़ा करके ये समझना होगा कि विज्ञान का मतलब सिर्फ रसायन नहीं। अगर अब वैज्ञानिकों ने अपनी ये सोच न बदली तो वे आने वाले समय में गैरज़रूरी हो सकते हैं।
(लेखक सेंटर फॉर सस्टेनबल एग्रीकल्चर के कार्यकारी निदेशक हैं। भारतीय शोध सेवा के वैज्ञानिक रह चुके हैं)
More Stories