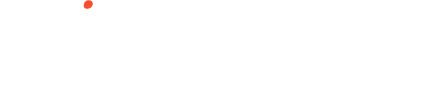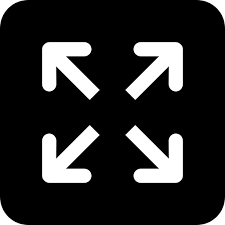कपास: नकदी फसल से विनाश की फसल
मराठवाड़ा के कपास के किसानों ने इनपुट - बीज, उर्वरक, बिजली, पानी - लागतों में निरंतर वृद्धि देखी है लेकिन राज्य का समर्थन न मिलने के कारण मुनाफा बहुत कम हो रहा है, जिससे कई किसान इस 'नकदी' फसल को छोड़ने पर मजबूर हैं...
 गाँव कनेक्शन 26 May 2018 9:21 AM GMT
गाँव कनेक्शन 26 May 2018 9:21 AM GMT
 प्रभाकर चव्हाल के परिवार ने कपास के लिए समर्पित क्षेत्र को कम कर दिया है, जिस पर अब वे अरहर, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी खाद्य फसलें उगा रहे हैं। फोटो- पार्थ एमएन / People's Archive of Rural India
प्रभाकर चव्हाल के परिवार ने कपास के लिए समर्पित क्षेत्र को कम कर दिया है, जिस पर अब वे अरहर, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी खाद्य फसलें उगा रहे हैं। फोटो- पार्थ एमएन / People's Archive of Rural Indiaप्रभाकर चव्हाल (30) का काम अपने चाचा, शिवाजी चव्हाल (55) की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। दोनों मराठवाड़ा के परभणी जिले के मोरेगांव में किसान हैं। दोनों मुख्यतः कपास का उत्पादन करते हैं, लेकिन शिवाजी का कपास जहां वर्षों से नकदी फसल रहा है, प्रभाकर की यही फसल अब ज्यादा नकदी नहीं लाती। इस मामले में चव्हाल अकेले नहीं हैं। मराठवाड़ा के परभणी, हिंगोली और औरंगाबाद जिले में वृहद स्तर पर कपास की खेती होती है - राज्य के कृषि विभाग के अनुसार, यहां 17.60 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती होती है। खाद्य फसलों जैसे ज्वार, अरहर और सोयाबीन की तुलना में कपास से ज्यादा आमदनी होती थी – इसी लिए कपास को 'नकदी' फसल कहा जाता है। हालांकि, गुजरते हुए वर्षों में कपास की उत्पादन लागत बढ़ी है, जबकि रिटर्न लगभग स्थिर रहा है, जिसके कारण कपास केवल नाम की नकदी फसल रह गई है।
प्रभाकर इसकी वजह विस्तार से बताते हैं। वह कागज का एक टुकड़ा निकालते हैं जिस पर उन्होंने सभी खर्चों को लिख रखा है जो कि उन्होंने एक एकड़ कपास की खेती करने में लगाए हैं – एक बोरी बीज के 800 रुपये, मध्य जून में बुवाई की मौसम से पहले खेत को तैयार करने के लिए मजदूरों को दी गई मजदूरी के 1,100 रुपये और बुवाई के समय 400 रुपये और। यदि मानसून में बारिश अच्छी रही, तो उन्हें तीन चरणों में घास को निकालने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए उन्हें 3,000 रुपये और मजदूरी के रूप में देने होंगे। उर्वरक? 3,000 रुपये और। कीटनाशक का मूल्य 4,000 रुपये। फसल कटाई की लागत 5,000 रुपये। और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अंतिम बाधा बाजार में इसे बेचने में आती है, जिसकी लागत 3,000 रुपये प्रति फसल है, जिसमें परिवहन तथा व्यापारियों को भुगतान किया जाने वाला कमीशन भी शामिल है। "इसमें प्रति एकड़ में 20,300 रुपये और जुड़ जाते हैं," प्रभाकर कहते हैं। इस साल प्रत्याशित बाजार दर, जब वह नवंबर-दिसंबर में अपने कपास की फसल काटेंगे, 4,300 रुपये प्रति क्विंटल है (पिछले साल यह 4,000 रुपये थी)। "आय [सभी लागत के बाद] 34,800 रुपये है," वे कहते हैं। अतः आठ महीने की कड़ी मेहनत तथा निवेश के बदले प्रति एकड़ मिले केवल 14,500 रुपये। इसके बाद चव्हालों को पानी के पंप, बोरवेल के लिए बिजली बिलों का भुगतान करना होगा - और उनकी छह गायों पर 14,000 रुपये से अधिक प्रति माह खर्च होते हैं।
रीब 15 साल पहले, शिवाजी चव्हाल 4,500-5,000 रुपये में एक एकड़ में कपास की खेती करने में सक्षम थे। । कीटनाशकों, उर्वरक और बीजों का मूल्य तब आज की तुलना में काफी कम था। कृषि श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में भी दोगुना से अधिक वृद्धि हुई है। बिजली के दाम भी बढ़े हैं। प्रभाकर का 15 सदस्यीय संयुक्त परिवार, उनके चाचा शिवाजी सहित, लगभग 30 एकड़ जमीन का मालिक है, जिसमें से 15 एकड़ कपास के लिए आरक्षित है। उन्होंने पिछले चार वर्षों में इसे घटाकर 7-8 एकड़ तक कर लिया है, जिसमें वह कपास की जगह अरहर, मूंग, उड़द तथा सोयाबीन जैसी खाद्य फसलें उगाते हैं। कपास एक प्यासी फसल है, जिसे खाद्य फसलों की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। मराठवाड़ा में 2012-2015 तक लगातार अकाल के चार वर्षों ने कपास की पैदावार पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। इस वर्ष भी, बारिश अच्छी नहीं हुई है। सूखे वर्षों ने किसानों को सिंचाई पर अधिक खर्च करने के लिए मजबूर किया है - बोरवेल ड्रिलिंग, पानी के टैंकरों की खरीद, या कुओं की खुदाई करके। हालांकि, कपास की कीमतों में समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। "कपास की बाजार दर [15 साल पहले] करीब 2,000 रुपये प्रति क्विंटल थी," चव्हाल कहते हैं। "एक एकड़ पर आठ क्विंटल उत्पादन का मतलब 16,000 रुपये था। तब इस पर 11,000 रुपये का मुनाफा था – अब हम 15 साल बाद जो मकाते हैं उससे सिर्फ 3,000 रुपये कम।"
कम कीमत के विभिन्न कारक हैं, जिसमें फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करते समय बढ़ते इनपुट लागत पर विचार करने से सरकार का इनकार भी शामिल है। अनुभवी कृषि नेता विजय जावंडिया के अनुसार, एक और कारण यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी कपास उत्पादकों के लिए काफी सब्सिडी है, जो कि भारत में उतार-चढ़ाव की घरेलू दर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। "इसके अलावा, गन्ना और कपास दोनों के नकदी फसल होने के बावजूद, उन पर अलग-अलग मापदंड लागू होते हैं," वे कहते हैं। "जब बाजार में बहुत अधिक मात्रा होती है, तो चीनी को सब्सिडी के साथ निर्यात किया जाता है, जिसकी वजह से कीमतों पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कपास निर्यात करने के लिए कोई सब्सिडी नहीं है। इसी प्रकार, चीनी पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क है, जबकि कपास पर कोई आयात शुल्क नहीं है।" "आज के सभी खर्चों को देख लीजिए," चव्हाल कहते हैं। "वे काफी ऊपर चले गये हैं। श्रमिक वर्ग [जैसे शिक्षक, सरकारी कर्मचारी या बैंक अधिकारी] के वेतन में वृद्धि को देखें और हमारे ग्राफ से तुलना करें। क्या यह उचित है?" जबकि कपास के किसानों को बढ़ती लागत और स्थिर रिटर्न के बीच निचोड़ा जा रहा है, घर पर कोई आपातकालीन स्थिति, परिवार में किसी की शादी या स्कूल की फीस की अतिरिक्त मात्रा भी उन्हें बैंक लोन के लिए आवेदन करने पर मजबूर कर सकती है, या इससे भी बदतर, किसी साहूकार के पास जाना पड़ सकता है, जो आम तौर पर प्रति माह 5% ब्याज लेता है।
प्रभाकर चव्हाल ने बैंक से जो 8 लाख रुपये ऋण लिये थे, उसमें से कुछ पैसे अपनी दो बहनों की शादी पर खर्च कर दिये, इस ऋण का अधिकांश भाग 2012-2015 के अकाल के वर्षों के दौरान लिया गया था; इस पैसों से परेशानी के इन वर्षों के दौरान परिवार को चलाने में मदद मिली। लेकिन चूंकि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा ऋण माफी की सीमा घटाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई है, प्रभाकर का परिवार माफी के लिए पात्र नहीं है। "मेरे पास साहूकार का कोई ऋण नहीं है," वे कहते हैं। "लेकिन आखिर यह कब तक चलेगा?" वर्ष 2006 में, स्वामीनाथन आयोग, जिसे कांग्रेस सरकार के निर्देशों पर कृषि संकट का आकलन करने और समाधान निकालने के लिए स्थापित किया गया था, ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके प्रमुख सुझावों में से एक यह था कि केंद्र सरकार किसानों को एमएसपी प्रदान करे जिसमें उत्पादन लागत में 50 प्रतिशत जोड़ कर कीमत तय की जाये। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। वर्ष 2014 में, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने कृषि क्षेत्रों में तेजी से अभियान चलाया, रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू नहीं किया। परभणी में स्थित एक वरिष्ठ पत्रकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता आसाराम लोमटे कहते हैं कि कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए अरहर या सोयाबीन जैसे विकल्प भी लाभकारी नहीं हैं, क्योंकि इन फसलों को भी उचित एमएसपी नहीं दिया जा रहा है, और ऐसी खाद्य फसलों पर रिटर्न अन्य फसलों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।
इसके अलावा, 15 साल पहले भारत में रुई के कीड़े को रोकने के लिए शुरू की गई आनुवंशिक रूप से संशोधित बीटी कॉटन को भी, अब कीटनाशकों की आवश्यकता है। "बीटी से पहले किसानों को कीटनाशकों पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता था," लोमटे कहते हैं। "वर्ष 2000 के बाद से, यह काफी कम हो गया। हालांकि, बीटी ने केवल 4-5 वर्षों तक अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद से, किसानों को फसल की बर्बादी रोकने के लिए कीटनाशकों का स्प्रे करने पर मजबूर होना पड़ा, और फिर से उनकी उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है।" परभणी के खुपसा गांव के रहने वाले 26 वर्षीय संतोष दसालकर का कहना है कि वह 2012 से ही कपास से कोई मुनाफा नहीं हासिल कर पाए हैं। "अब [अगस्त] तक फसल कमर के आसपास होनी चाहिए," उन्होंने कहा, लेकिन यह मुश्किल से टखने तक पहुंच रही है। "यहां तक कि अगर मानसून के बाकी दिनों में अच्छी बारिश होती है, तो भी इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि मैं एक एकड़ से तीन क्विंटल से ज्यादा कटाई कर सकूं। पिछले साल को छोड़ कर, 2012 के बाद से ही यह कहानी चली आ रही है।" दसालकर के पास परभणी-शेलू राजमार्ग के पास एक 7 एकड़ का खेत है, जिसमें से पांच एकड़ कपास की खेती के लिए है। उनके दो बच्चे हैं, जिनकी आयु छह साल और आठ साल है, जो एक नगरपालिका स्कूल में पढ़ रहे हैं। "प्राइवेट स्कूल डोनेशन के रूप में 5,000 रुपये मांगते हैं," वे बताते हैं। "और यहां मेरे ऊपर 2 लाख रुपये का बैंक ऋण है।" वर्ष 2015 में भी जब सूखा पड़ा, तो उसके बाद संतोष की पत्नी सविता दसालकर ने बुवाई के लिए पैसा इकट्ठा किया। "हमने एक लोन कंपनी के पास 70,000 रुपए के अपने स्वर्ण आभूषणों को गिरवी रख दिया और उससे 40,000 रुपये प्राप्त किए," वह कहती हैं। "इसके बिना, हम बुवाई नहीं कर पाते। सोने के आभूषण मेरी शादी के समय बनवाये गये थे। हम अभी भी इसे वापस प्राप्त नहीं कर सके हैं। बात यह है कि जब भी हमें लाभ होता है, तो सिर्फ थोड़ा होता है लेकिन जब हानि होती है, तो बहुत अधिक होती है।"
हिंदी अनुवादः डॉ. मोहम्मद क़मर तबरेज़
'This article was originally published in the People's Archive of Rural India on March 28, 2018 मूल ख़बर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें
Next Story
More Stories