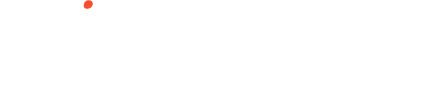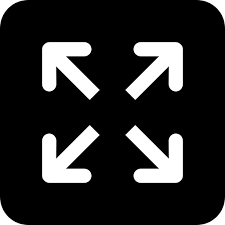भारत में भी वोट डालने के साथ चुनाव के नतीजे घोषित क्यों नहीं हो सकते?
ईवीएम मशीनों के साथ यदि कोई कठिनाई है तो, वह है देश का अनेक सप्ताहों तक चलने वाला चुनाव और बैलेट बाक्सों की लंबे समय तक रखवाली। अमेरिका जैसे देशों में वोट जैसे-जैसे डाले जाते हैं, उसी के साथ उनकी गणना होती रहती है। इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहती मतदाता के वोट डालने के बाद कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं होती होगी।
 Dr SB Misra 25 May 2024 5:30 AM GMT
Dr SB Misra 25 May 2024 5:30 AM GMT

अभी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के कुछ समय पहले चुनाव प्रक्रिया पर तीखी बहस जारी थी, ईवीएम की लगातार बुराई हो रही थी और उन पर नाराज़गी जताई जा रही थी। चुनाव की यह प्रक्रिया दशाब्दियों के अनुभव के बाद विकसित हुई है, इसमें कोई गंभीर दोष भी नहीं मिला है। इन्ही मशीनों के बल पर विपक्ष के तमाम लोग कह रहे हैं, कि इस बार मोदी पराजित हो जाएँगे और मोदी जी भी कह रहे हैं, कि “अब की बार 400 पार”।
ईवीएम मशीनों के साथ यदि कोई कठिनाई है तो, वह है देश का अनेक सप्ताहों तक चलने वाला चुनाव और बैलेट बाक्सों की लंबे समय तक रखवाली। अमेरिका जैसे देशों में वोट जैसे-जैसे डाले जाते हैं, उसी के साथ उनकी गणना होती रहती है। इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहती मतदाता के वोट डालने के बाद कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं होती होगी।
60 के दशक में जब कनाडा के वर्तमान प्रधानमन्त्री के पिता पियर एलियट ट्रूडो वहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए थे, तब मैं वहीं था। और इस दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी चुने गए थे, उस चुनाव को भी मैंने देखा था। दोनों ही चुनाव में कोई हल्ला-गुल्ला नहीं दिखा, जो शोर-शराबा और लाउडस्पीकर की आवाज़ भारत में देखी थी। इस समय रूस के एक पत्रकार से किसी ने पूछा, कि आपके यहाँ प्रजातंत्र है, क्या? उसने कहा था हाँ! है, तो फिर आगे उसने पूछा, कि चुनाव कैसे होते हैं, आपके वहाँ, तो उसने उत्तर दिया ‘’नाइस एंड पीसफुल’’।
एक तो भारतीय चुनाव की अपेक्षा शोर-शराबा की कमी और दूसरे जिस दिन चुनाव हुआ उसी रात चुनाव के परिणाम आ गए थे। मेरे लिए यह एक सुखद आश्चर्य था और आज भी है, कि वह दिन कब आएगा जब हफ्तों-हफ्तों वोटों की पर्चियों से भरे हुए बक्सों की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी और परिणाम यथा-शीघ्र आ जाया करेंगे। विकसित प्रजातांत्रिक देश में वोट डालने की मशीन में एक तरफ वोट डाले जाते हैं तो उसके साथ ही गिनती करने वाली मशीन में डाले गए वोट जुड़ते जाते हैं, इस प्रकार चुनाव का परिणाम अविलम्ब घोषित हो पाता है। शासक चुनने की प्रक्रिया बहुत पुरानी है, लेकिन तरीका बदलता रहा है।
हमारे देश में शासक चुनने के लिए संघर्ष या खून-खराबा नहीं होता था, बाहर से आए हुए लोगों ने यह परम्परा भले ही डाली हो। शासक अगर अपने प्रजा के विचारों और भावनाओं का ध्यान रखें तो वह प्रजातन्त्र की मूल भावना को लेकर चल रहा होगा। हमारा आदर्श ‘रामराज्य’ को माना जाता है, जिस जमाने तक पुरुष ही शासक होता था, सबसे बड़ा बेटा ही राजगद्दी पर बैठता था। जब रामचंद्र जी को वनवास जाने का समय आया तो उनके छोटे भाई भरत को राजगद्दी पर बिठाने का प्रस्ताव हुआ। इसके विपरीत सभी संस्कृतियों में शासक संघर्ष के द्वारा चुना जाता रहा है।
औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को जेल में बन्द कर दिया और भाई दारा शिकोह को फांसी पर चढ़ाकर रास्ते से हटा दिया। यह थी मध्य पूर्व की परम्परा, जो भारत में मुगलों के आने के पहले कभी नहीं रही। मुगलों के समय में सहज और स्वाभाविक सत्ता परिवर्तन देखने को कम ही मिलता है। सत्तासीन पिता या भाई को किसी न किसी प्रकार हटाकर बादशाहों ने सत्ता हासिल की थी। इसके विपरीत भारत सनातन परम्परा में, सत्ता! स्वाभाविक रूप से सबसे बड़े बेटे को सहज ढंग से सौंप दी जाती थी।
यदि पहली बेटी हो, तो अगले बेटे को सत्ता दी जाती थी। रामचन्द्र जी को सत्तासीन करने की पूरी तैयारी हो गई थी लेकिन उन्हें, वनवास जाना पड़ा और उनके स्थान पर उनके छोटे भाई भरत को नामित किया गया। भरत ने विनम्रता पूर्वक यह ज़िम्मेदारी स्वीकार तो कर ली लेकिन राजगद्दी पर कभी नहीं बैठे।
वह बड़े भाई श्री राम के चरण पादुकाओं को सत्तासीन करके राम के पद चिन्हों पर चलते हुए 14 वर्षों तक शासन चलाते रहे। भारत में राजचन्द्र व्यवस्था बहुत ही स्नेह भाव से राजा द्वारा चलाई जाती थी और राजा अपने प्रजा को पुत्रवत मानता था। राजा सहृदय भी होता था उसके मन में कुंठा का भाव तनिक भी नहीं रहता था। जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय पाई और कलिंग राज्य की प्रजा की लाशों के ढेर लग गए, तो यह दृश्य देखकर अशोक का दिल दहल गया और उसने भविष्य में कभी भी युद्ध न करने का फैसला लिया। इतना ही नहीं उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उसके प्रचार-प्रसार में जुट गया तथा अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका को बौद्ध धर्म का शांति संदेश लेकर भेजा।
रामराज्य का आदर्श हमारे सामने तो है ही लेकिन सम्राट हर्षवर्धन हर 5 साल के बाद अपना सब कुछ प्रजा को दान कर देता था और यहाँ तक कि अपनी बहन राज्यश्री से कपड़े माँग कर पहनता था, क्या किसी देश में ऐसे राजतन्त्र की कल्पना की जा सकती है? हमारे देश से तमाम लोग विदेशों को भ्रमण करने के लिए गए थे वह साथ में अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं गए बल्कि वे अपने साथ सत्य, अहिंसा और शान्ति का सन्देश लेकर दुनिया के कोने-कोने में पहुँचे थे। इस प्रकार की शांति और अहिंसा का नुकसान यह हुआ कि हमारे देश में धर्म के ज्ञाता और प्रवर्तक तो पैदा हुए लेकिन धर्म रक्षक नहीं पैदा हुए।
परिणाम देश की दौलत और सम्पदा पर बाहर रहने वाले आतताइयों, अत्याचारियों की नजर पड़ी और समय-समय पर आक्रमण करके देश को लूटते रहे। दूसरे धर्म के मामले में शासक ही धर्म प्रचार करने वाला होता था और धर्म का विस्तार तलवार के बल पर हुआ करता था। हमारे देश में धर्म प्रचारक विद्वान, सन्यासी और ऐसे ही शान्ति प्रेमी लोग होते थे और यहाँ तक कि राजा भी ऐसे विद्वानों की सलाह से ही राज्य चलाता था।
तमाम देशों में शासन का फैसला उसी सिद्धान्त के आधार पर होता रहा है, जिसमें कहा गया “वीर भोग्या वसुन्धरा” अर्थात जिसकी “लाठी उसकी भैंस”। अमेरिका जैसे देश में भी हुड़दंग करने वाले घूमते रहते थे, यह तब की बात है जब वहाँ प्रजातन्त्र स्थापित नहीं हुआ था और इन लोगों को यांकी भी कहते थे और जो इधर-उधर लूटपाट मचाया करते थे। लेकिन अमेरिका में अन्य पश्चिमी देशों के मुकाबले प्रजातन्त्र पहले आया था और उस देश में दुनिया के सभी भागों से आए हुए लोग बसते रहे हैं। भारत के प्रजातांत्रिक राज्यों का इतिहास तो पता नहीं है, इसलिए अमेरिका का प्रजातंत्र सबसे पुराना और भारत का प्रजातंत्र सबसे बड़ा कहा जाता है। वैसे ग्रीस में सुकरात और प्लेटो जैसे महान विचारक पैदा हुए थे, लेकिन ग्रीस के इतिहास के विषय में सिकन्दर के अलावा अधिक जानकारी नहीं है। लेकिन अन्य देशों में या तो तानाशाही अथवा कुछ लोगों द्वारा क्रांति का रास्ता अपनाकर साम्यवाद की स्थापना की गई।
कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर रूस में लेनिन और फिर स्टालिन ख्रश्चन आदि ने साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की थी। वहाँ साम्यवादी व्यवस्था के पहले जिन लोगों का शासन था उनके संभावित: आम जनता संतुष्ट नहीं थी। साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना में चीन में माओ त्से तुंग ने बड़ी भूमिका निभाई और उस संघर्ष में चाहे रूस हो या चीन तमाम आम आदमी मर गए। चाहे एक आदमी की तानाशाही हो अथवा एक ग्रुप का शासन हो, साम्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत दोनों में ही आम जनता के व्यक्तिगत आजादी को कोई स्थान नहीं होता जो भी शासन चलाता है उसी के अनुसार व्यवस्था स्थापित होती है।
प्रजातांत्रिक व्यवस्था मानवीय परिपक्वता का परिणाम है और इसे फ्रांस के रूसो नाम के विचारक ने कहा था “लोगों के लिए लोगों से और लोगों द्वारा स्थापित की जाने वाली व्यवस्था प्रजातांत्रिक होती है”। फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कमियाँ या खामियाँ नहीं है, इसमें भी बहुत सी कमियाँ हैं, जब प्रजातांत्रिक तरीके से हमारे देश में चुनाव आरम्भ हुए तो सबसे पहले 1947-48 में पंचायत के चुनाव हाथ उठाकर कराए गए थे।
मुझे याद है ठाकुर छत्रपाल सिंह के दरवाजे पर तमाम महिलाएँ इकट्ठा हुई थी और कुछ अधिकारी आए थे, जो प्रत्याशी का नाम पुकार कर हाथ उठवाते थे और संख्या लिख लेते थे। वह चुनाव तो सम्पन्न हो गया, लेकिन भारत के गणराज्य का चुनाव 1952 में कराया गया। इस बार पर्चियाँ छपी थी, मगर सारी पर्चियाँ एक जैसी थी केवल अंतर यह था कि जो बैलट बॉक्स थे उनके ऊपर पार्टियों के चुनाव चिन्ह छपे हुए थे और अपने मनपसंद चुनाव चिन्ह वाले बैलट बॉक्स में वोट की पर्ची डालनी होती थी।
बहुत लोग पर्ची बैलट बॉक्स के अन्दर डालने के बजाय उसके सामने ही डालकर आ गए थे और कुछ होशियार लोग जैसे हमारे गाँव के जानकी प्रसाद मिश्रा जब गए तो सारे बैलेट बॉक्सो के सामने पड़ी हुई पर्चियाँ बटोर कर दो बैलों की जोड़ी के निशान वाले बैलेट बॉक्स में डाल दिए यह उन्होंने खुद ही बताया था।
इस चुनाव में वोटिंग की गिनती करते समय बहुत सी गड़बड़ियां सामने आई थी; जैसे गिनती के समय बिजली का चला जाना और फिर पर्चियों को एक बक्से से दूसरे बक्से में डाल देना यह सामने आया था। इन अनुभव से सीख लेकर 1957 में दूसरे आम चुनाव में बहुत से सुधार किए गए थे। एक सुधार तो यह था कि पर्चियों पर पार्टियों के चुनाव चिन्ह छापे थे और उस पर्ची पर मनचाहे चुनाव चिन्ह पर मोहर लगानी होती थी। इसमें पर्चियों की हेरा फेरी की आशंका काफी हद तक घट गई थी, लेकिन जहाँ हेरा फेरी की गुंजाइश थी वहाँ केवल काँग्रेस को ही लाभ मिलता था, क्योंकि उसका ही वर्चस्व था। 1962 में तीसरा आम चुनाव हुआ और तब वोटर की उंगली पर स्याही लगाई जाने लगी, जो आसानी से मिटती नहीं थी और कोई आदमी दोबारा वोट नहीं डाल सकता था। इन तमाम अनुभवों के बाद हमारा प्रजातंत्र धीरे-धीरे परिपक्व होता चला गया और 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी पराजय का मुँह देखना पड़ा। प्रांतीय स्तर पर देश में अनेक प्रांतों में संयुक्त
विधायक दल के नाम से गैर काँग्रेसी सरकारें बनीं लेकिन अपने अंतर-विरोधों के कारण वह सरकारें अधिक समय चल नहीं पाई। केंद्र में काँग्रेस की सरकार बनी रही, लेकिन अन्तत: कांग्रेस के दो भाग हो गए, एक तो काँग्रेस (ओल्ड) और दूसरी काँग्रेस (आई), उनके अलग-अलग चुनाव चिन्ह थे।
1971 में भारत के हाथों पाकिस्तान की बड़ी पराजय हुई और पाकिस्तान के दो खंड हो गए, पश्चिमी पाकिस्तान और बंगला देश। इस विजय का श्रेय इंदिरा गाँधी को मिला और 1972 में बम्पर वोटो से उनकी विजय हुई। लेकिन न्यायपालिका ने अपना फैसला उनके चुनाव के विरुद्ध सुना दिया और इंदिरा जी का चुनाव रद्द कर दिया। इस प्रकार न्यायाधीश सिन्हा जी ने एक इतिहास रच दिया जिसमें प्रजातांत्रिक ढँग से चुने गए सदस्य को टेक्निकल ग्राउंड पर अयोग्य घोषित किया गया था। इंदिरा जी ने न्यायालय के इस फैसले को नहीं माना और मतपत्रों के माध्यम से चुनी गई सरकार ने आपातकाल जून 1975 में घोषित कर दिया।
यह आपातकाल की घोषणा वास्तव में दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के माथे पर एक कलंक का धब्बा बन गया। इसके बाद चुनाव होते गए, चुनाव सुधार भी होते रहे, सरकारें आती रहीं, सरकारें जाती रहीं। आखिर वर्तमान चुनाव पद्धति आई जिसमें ईवीएम मशीन द्वारा मतदान का प्रावधान बना है। कुछ लोग इस व्यवस्था को ठीक नहीं मानते और वह व्यवस्था ठीक मानते हैं जब हाथ से मोहर लगाई गई पर्ची वोट के रूप में डाली जाती थी और उसी के साथ लठैतों की मसल्स पावर का भरपूर प्रयोग होता था। शायद यह लोग वही पुरानी लठैतों वाली व्यवस्था चाहते हैं, जो प्रजातंत्र के ऊपर, आपातकाल से बड़ा कलंक होगा ।
भ्रष्टाचार हमारे प्रजातांत्रिक ढाँचे को हमेशा से कमजोर करता आया है। पहले कम्पनियाँ, व्यापारी आदि पार्टियों को बराबर चन्दा देते थे, लेकिन सरकार में जो पार्टी होती थी, उसे सबसे अधिक चन्दा मिलता था और उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं रहता था। अब हिसाब किताब रहे और कुछ हद तक पारदर्शिता बनी रहे इसलिए चुनावी बॉण्ड शुरू किए गए थे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों से लेकर न्यायाधीशों तक ने इस व्यवस्था को ख़ारिज कर दिया है। केवल इस तरह चन्दा लेने की बात ही नहीं है, बल्कि बाहुबली कितने लोगों से जबरन चंदा वसूल करते आए हैं इस पर भी कोई अंकुश नहीं था।
हमारे चुनाव संचालन का एक दोष यह भी है जिसमें स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों की बसों को चुनाव टीम के लिए जबरदस्ती ले लिया जाता है । कहीं भी शिकायत करने पर सुनवाई नहीं होती, इतना ही नहीं चुनाव से चार दिन पूर्व अधिग्रहित की गयी बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए खाने अथवा नास्ते की उचित व्यवस्था नहीं की जाती, ऐसी जानकारी वर्तमान में हो रहे चुनाव में गए ड्राइवर और कंडक्टरों से मिली है। ध्यान रहे प्राइवेट विद्यालयों को जो लोग बसे दान में देते हैं वह विद्यार्थियों को घर से स्कूल और वापस घर तक ले जाने के लिए देते हैं। मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग के पास पैसे की इतनी तंगी तो नहीं है, कि वह किराए की बसें या सरकारी बसें ना ले सके। यह भी मेरे विचार से एक प्रकार का अनुचित तरीका है, इस पर कोई अंकुश लगा पाना सम्भव नहीं रहेगा।
आजकल एक मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया जा रहा है और वह है जातीय गणना। ऐसा लगता है कि कुछ जातियाँ अमीर हैं कुछ गरीब है और इससे विकास को गति मिलेगी, कितने नादान हैं वे लोग? जातियाँ ऊँचे और नीचे को छोटे और बड़े को तो व्यक्त करती हैं लेकिन धनी और निर्धन का भेद नहीं करती। हर जाति में गरीब हैं और हर जाति में अमीर हैं, यदि सेकुलर पैमाना अपनाना हो तो निर्धनता का पैमाना ढूँढना होगा, जैसे साम्यवाद में होता है वह कहते हैं; “प्रोलिटेरिएट (दरिद्रतम श्रमिक वर्ग) ऑफ़ द वर्ल्ड यूनाइट”, लेकिन यदि उन हजारों साल के पूर्वाग्रह और विदेश को लेकर जातीय गणना कराई गई, तो उसका परिणाम उतना ही या उससे अधिक खराब होगा, जितना पञ्चायती चुनाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। चन्द वोटों के लिए सम्पूर्ण भारतीय समाज को छिन्न-भिन्न, नेस्तनामूद करने का प्रयास न हो तो अच्छा है।
जातियों के पीछे जो भावना थी, जो मूल विचार था, वह यह था कि जो गन्दा आदमी है उसे सामाजिक जाति की सीढ़ी से नीचे उतारा जाता था और निचले पायदान वाला निचली जाति वाला कोई अगर अच्छा काम करता था तो उसे ऊँची जाति का घोषित कर दिया जाता था। यह सामाजिक नियंत्रण के लिए एक तरह लीवर का काम करता था, लेकिन आज के युग में ना तो इसकी आवश्यकता है और ना यह सफल होगा।
चुनावों में अब अगर कोई सुधार होना है तो वह यही होना चाहिए जैसे अमेरिका में या कनाडा में होता है, कि मतदान और मतों की गणना साथ-साथ चले और चुनाव परिणाम यथा-शीघ्र घोषित हो जाएँ । मत पेटियों की सुरक्षा और उन्हें हफ्तों-हफ्तों बचाना, यह तो बंद होना ही चाहिए। आशा है इस प्रकार के सुधार होंगे और ईवीएम की दिशा में बढ़ाया गया कदम पीछे नहीं हटेगा।
Gaon Postcard
More Stories