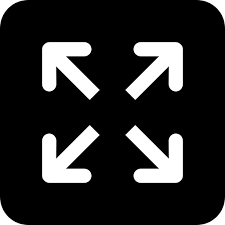मिट्टी, पानी, हवा बचाने के लिए याद आई पुरखों की राह
खेती की पुरानी विधाएं फिर से अपनाने और आधुनिक पद्धतियों को त्यागने से भी काम नहीं चलेगा। हमें पुरातन को युगानुकूल और विदेशी का स्वदेशानुकूल बनाकर चलना होगा अन्यथा दुनिया में बहुत पिछड़ जाएंगे। सीरीज 'खेती में देसी क्रांति' का पहला हिस्सा…
 Dr SB Misra 16 Jan 2019 6:15 AM GMT
Dr SB Misra 16 Jan 2019 6:15 AM GMT

सीरीज की पहली ख़बर यहां पढ़ें-जलवायु परिवर्तन और कंपनियों का मायाजाल तोड़ने के लिए पुरानी राह लौट रहे किसान?
कुछ मजबूरी और कुछ लालच में किसानों ने विदेशी विधियां अपनाकर पचास साल खेती किया और अपने खेतों की मिट्टी, जमीन के अन्दर का पानी और वातावरण की हवा प्रदूषित कर ली। अन्नदाता की मजबूरी बनी देश की आबादी जो 1955 में केवल 40 करोड़ थी और आज 136 करोड़ हो गई है। अन्नदाता क्या करता, अपने परिवार का पेट भरना था और देश का भी। साठ के दशक में भुखमरी की नौबत आ गई तो इन्दिरा गांधी की सरकार ने किसानों पर लेवी लगा दिया, जिसका मतलब था जमीन के रकबा के हिसाब से सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूं की एक निश्चित मात्रा जमा करनी थी, अन्यथा सजा का प्रावधान था।
उन्हीं दिनों बाजार में नार्मन बॉर्लाग नामक वैज्ञानिक की टीम द्वारा विकसित अधिक उपज देने वाली बौनी प्रजाति का गेहूं और धान आया जिसकी किसान को अत्यन्त आवश्यकता थी।
बौनी प्रजातियों की पैदावार पारम्परिक गेहूं से कई गुना अधिक थी और किसानों ने पैदावार पूरी लेने के लिए यूरिया झोंकना आरम्भ कर दिया। बाद में लेवी वसूली बन्द हो गई, लेकिन किसान का लालच नहीं बन्द हुआ। जो मैक्सिकन गेहूं वरदान बनकर आया था, अन्ततः अभिशाप बन गया। यह गेहूं कई गुना अधिक पैदावार देता है फिर भी गिरता नहीं है, लेकिनु इसमें पानी और खाद की अधिक आवश्यकता होती है।
यह भी पढ़ें: पानी की इस बंपर फसल में से किसान के लिए बचेगा कुछ?
फिर आईं धान की नई-नई प्रजातियां जिनमें बौने धान की आईआर-8 किस्म प्रमुख थी। भारत के किसानों ने अपनी पुरानी किस्में भूलकर गेहूं और धान की नई प्रजातियों को अपना लिया, इसे हरित क्रान्ति कहा गया।
निरन्तर पैदावार बढ़ाते रहने के प्रयासों से रासायनिक खादों का उपयोग खूब बढ़ा और फसलों में बीमारियां भी बढ़ीं। बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए कीटनाशक, फफूंदनाशक और ना जाने कितने प्रकार के इन्सेक्टीसाइड और पेस्टीसाइड प्रयोग होने लगे। दवाइयां छिड़कते रहे, बीमारियां बढ़ती रहीं। पानी की अत्यधिक मांग के कारण भूजल पर दबाव बढ़ा और जलस्तर गिरता गया, पेस्टीसाइड और इन्सेक्टीसाइड के अधिक प्रयोग से कैंसर जैसी बीमारी फैल रही है और रासायनिक पदार्थों के विकिरण से हवा जहरीली हो रही है।
खेती अब जीवन यापन का जरिया न होकर व्यावसायिक रूप ले रहीं थी, किसान का लालच भी बढ़ रहा था। सत्तर के दशक में तो किसानों को लगा हम जितना यूरिया डालते जाएंगे, पैदावार बढ़ती जाएगी, लेकिन यह ज्यादा समय नहीं चला। एक समय आया जब यूरिया बढ़ाने के बाद भी पैदावार बढ़नी बन्द हो गई। पता चला कि यूरिया तो पौधे को केवल नाइट्रोजन देती है, उसे फास्फोरस और पोटाश भी चाहिए।
तब किसानों ने एनपीके अर्थात नाइट्रोजन-फास्फोरस-पोटाश डालना शुरू कर दिया। अनेक स्थानों पर एनपीके की मात्रा बढ़ाते रहने के बावजूद प्रति एकड़ पैदावार बढ़नी बन्द हो गई।
यह भी पढ़ें: किसान का मर्ज़ खैरात के पेनकिलर से नहीं जाएगा
वैज्ञानिकों ने बताया कि अकेले एनपीके पर्याप्त नहीं है। जब खूब खाद डालते हो तो तन्दुरुस्त पौधों को उसी अनुपात में विविध सूक्ष्म तत्व या खनिज जैसे लोहा, तॉबा, कैल्शियम, सल्फर, जस्ता, मैग्नीशियम आदि की भी जरूरत बढ़ जाती है और पौधा जमीन से इन तत्वों को घसीटता है।
उदाहरण के लिए जब दुधारू गाय को इंजेक्शन लगाकर दूध निकालते जाते हैं तो उसका शरीर टूटता जाता है उसी प्रकार धरती से उर्वरा शक्ति खींचते रहने से धरती बांझ होने होने लगी है। इसके विपरीत जब धीरे-धीरे पौधे इन तत्वों को लेते हैं तो प्रति वर्ष मिट्टी छीजने या रिसने से सूक्ष्म तत्व मिट्टी में बनते रहते हैं।
आज कल कुछ लोग कहते हैं बहुफसली खेती करनी चाहिए मानों कोई आविष्कार किया हो। इस देश में जब पुरानी प्रजातियां बोई जाती थीं तो किसान मिली-जुली खेती करता था, जैसे गेहूं-सरसों, चना-अलसी-सरसों, अरहर-उरद, ज्वार-अरहर, अरहर-उरद और ना जाने कितने मिश्रण बनाकर बोए जाते थे।
बौनी प्रजातियां आने के बाद एकल प्रजाति (मॉनो क्राप) में तात्कालिक लाभ दिखाई पड़ा और बहुफसली खेती केा बन्द कर दिया गया। पौध विविधता कम होने लगी और अनेक प्रजातियां तो विलुप्त हो गई या हो रही हैं। वास्तव में बहुफसली खेती के बहुत लाभ थे और इस ओर फिर से वैज्ञानिकों और किसानों का ध्यान जा रहा है।
विदेशों से एक और समस्या आई उन्नत बीजों के साथ। अनेक प्रकार के खर पतवार के बीज भी आ गए जो स्थानीय उत्पत्ति के नहीं हैं और जिनके बारे में हमने सुना तक नहीं था। उन्हें भी नष्ट करने के लिए विषैली दवाओं का प्रयोग होता है, जो हवा, पानी और मिट्टी के जरिए आदमी के शरीर में पहुंच रही हैं। बैक्टीरिया, फफूंद, वाइरस, यहां तक कि कीड़े-मकोड़े भी विषवरोधी अर्थात इम्यून हो गए हैं। उन पर विष का असर नहीं होता। कहना कठिन है कि धरती को धीरे-धीरे बांझ और पर्यावरण को विषैला बनाने में हरित क्रान्ति को दोषी माना जाए या फिर लालची किसान को।
यह भी पढ़ें: बजट में किसानों की मर्ज़ का उपचार हुआ, लेकिन किस मर्ज़ का ?
आप ने उस मुर्गी की कहानी सुनी होगी जो रोज सोने का एक अंडा देती थी। लालची मालिक ने सोचा क्यों ना एक साथ सब अंडे निकाल लें और मुर्गी को ही मार डाला। यदि उसके पास कोई यंत्र होता यह जानने का कि मुर्गी के पेट में और कितने अंडे बचे हैं तो शायद न मारता। अब किसान को साधन उपलबध हैं मिट्टी की जांच कराने के जिससे पता लग जाता है इसमे कितनी जान बची है अथवा कितने तत्वों की कमी आ गई है।
अब लोगों को जैविक खेती याद आई है जिसे पचास साल पहले त्याग दिया था और कीटनाशकों के रूप मे नीम, लहसुन, मदार जैसे पदार्थों का प्रयोग आरम्भ हो चुका है। वह विधाएं जो देश में सैकड़ों साल से प्रचलित थीं, पुनर्जीवित हो रही हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहां प्रतिवर्ग किलोमीटर 455 लोग रहते हैं, वहां अन्न का उत्पादन जीवन यापन के लिए ही होना चाहिए न कि निर्यात के लिए। जिस देश में कभी 'उत्तम खेती, मध्यम बान, निपट चाकरी भीख समान' का सोच था, वहां अब खेती को व्यापार बना रहे हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरह जहां आबादी का दबाव है ही नहीं ।
हमें चीन की तरह देश की आबादी घटाने का युद्धस्तर पर प्रयास करना होगा नहीं तो बहुफसली खेती, जैविक खेती या नई प्रजातियों की खेती हमारा उद्धार नहीं कर पाएगी। खेती की पुरानी विधाएं फिर से अपनाने और आधुनिक पद्धतियों को त्यागने से भी काम नहीं चलेगा। हमें पुरातन को युगानुकूल और विदेशी का स्वदेशानुकूल बनाकर चलना होगा अन्यथा दुनिया में बहुत पिछड़ जाएंगे।
यह भी पढ़ें: भूखी-प्यासी छुट्टा गाएं वोट चबाएंगी, तुम देखते रहियो
More Stories